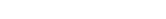वियोजन की संरचना कुछ इस तरह से की जानी चाहिए ताकि वंचित वर्ग के हितों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सके. कई दशकों से समाज विज्ञान इस प्रश्न से जूझता रहा है, लेकिन इस विषय पर अधिकतर शोध-कार्य कोटे के विशिष्ट स्वरूप पर ही केंद्रित रहा है. लेकिन अनिवार्य कोटा, भले ही वह राजनीति से संबंधित हो या शिक्षा से या निजी क्षेत्र से संबंधित हो सिर्फ़ एक प्रकार के कोटे को ही दर्शाता है. यह एक प्रकार का समावेशन है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को मौजूदा संस्थाओं में प्रवेश मिलता है या वर्णनात्मक और ठोस प्रतिनिधित्व के ज़रिये हाशिये पर पड़े वर्गों को इन संस्थाओं में उनके उच्चतम स्तर पर मुख्य धारा में प्रवेश मिलता है.
और कुछ अन्य प्रकार के काल्पनिक प्रतिनिधित्व भी हैं. इनमें ऐसे प्रतिनिधित्व भी हैं जो समावेशन के बजाय मूलतः वियोजन में निहित हैं. संरचनाओं में राज्य की ओर से एक ऐसे समूह-विशिष्ट तंत्र की स्थापना की जाती है, जिसमें वंचित समुदाय को केवल समूह में ही समायोजित किया जाता है. उदाहरण के रूप में राजनीति में समूह-विशिष्ट व्यवस्थाओं के अंतर्गत वियोजित (संयुक्त के विपरीत) निर्वाचक मंडल को शामिल किया जाता है ताकि (क) कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में विशिष्ट समुदाय के लिए ही आरक्षण किया जा सके और (ख) अल्पसंख्यक मतदाता ही उन निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए अपना मतदान कर सकें. वस्तुतः यह व्यवस्था सन् 1909 में भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए की गई थी और बाद में अल्पसंख्यक समुदाय के नेता इसे जातिगत सशक्तीकरण और सामाजिक विकास के साधन के रूप में अपनाने लगे.
आजकल वियोजित या समूह-विशिष्ट प्रतिनिधित्व चुनावी व्यवस्था में लगभग न के बराबर है. फिर भी आपराधिक न्याय के क्षेत्र में यह तरकीब चलने लगी है. इसके परिणामस्वरूप हमारे पास कुछ आधुनिक उदाहरण भी हैं, जिनसे इस वैकल्पिक व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष की कल्पना की जा सकती है. बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक दक्षिण में स्थित ब्राज़ील जैसे देशों से लेकर भारत तक के देशों ने वियोजन के इस विचार को आपराधिक न्याय के क्षेत्र में केवल महिलाओं द्वारा संचालित संस्थाओं का गठन करके महिलाओं के सशक्तीकरण की योजना को पुनर्जीवित किया है और इसके अंतर्गत इसी विशिष्ट समुदाय द्वारा पुलिस थानों का संचालन किया जाता है और इससे यही विशिष्ट समुदाय ही लाभान्वित हो सकता है. इस समय भारत में केवल महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस थानों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है. इसके अलावा समुदाय विशेष द्वारा अन्य संस्थाएँ भी शुरू की गई हैं, जैसे महिलाओं की अदालतें, अनुसूचित जाति / जनजाति के पुलिस थाने (जिनका संचालन भी इसी जातिगत समुदाय द्वारा किया जाता है और ऐसे थानों में इसी समुदाय के मामले ही निपटाये जाते हैं). इसी प्रकार अन्य उपाय भी किये गए. वियोजन की संस्था के पीछे भावना यही है कि कोटे और वियोजन के अन्य काल्पनिक तौर-तरीके अपनाने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अभी भी प्रताड़ित हो सकता है. इसलिए उनकी अपनी संस्थाओं के अंदर ही कानूनी या समुदायों के संस्थागत या “एन्क्लेवों” के वियोजन से न केवल सैद्धांतिक रूप में सेवा मिल सकेगी, बल्कि भेदभाव और पक्षपात से भी अलग रहकर उनका बचाव हो सकेगा.
कई आलेखों में मैंने वियोजन के रूप में प्रतिनिधित्व के साथ संबद्ध गतिविज्ञान की छान-बीन की है. मैंने यह छान-बीन उत्तर भारत में स्थित पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस थानों के नज़रिये से की है. अपने पहले अध्ययन में मैंने यह स्पष्ट किया है कि वियोजन के प्रतिनिधित्व की संरचना में ही अल्पसंख्यकों का वियोजन भी निहित है. अल्पसंख्यक प्रशासकों के वियोजन और लैंगिक सरोकार के कारण खास तौर पर परंपरागत सामाजिक प्रतिमानों के परिवेश में अनचाहे ही कई दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं. सूक्ष्म स्तर पर अपराध के आँकड़ों और अन्य प्रकार की सूचनाओं के स्रोतों का उपयोग करते हुए मैंने दर्शाया है कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित निकायों की स्थापना से अन्य संस्थाओं (अर्थात् सामान्य पुलिस थानों) को भी शिकायतकर्ताओं को आगे बढ़ा देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है. इसके फलस्वरूप लैंगिक सरोकारों के मामलों को “मुख्य धारा” की पुलिस व्यवस्था से अलग हटाकर एक सीमित दायरे में ढकेल दिया जाता है. इसके अलावा, चूँकि महिला प्रशासकों को केवल लैंगिक मामले ही सौंपे जाते हैं, इसलिए उनकी क्षमता का विकास नहीं हो पाता (अर्थात् हत्या या अपहरण जैसे मामलों की छानबीन करने जैसे मामले उनके पास नहीं आते). मेरा सुझाव है कि यह विडंबना ही है कि पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देकर “एन्क्लेव” सामूहिक विषमताओं को बढ़ावा दे सकते हैं और इन क्षेत्रों की तुलना में केवल महिलाओं द्वारा संचालित निकायों का मूल्यांकन किया जाता है. एक अन्य अध्ययन में मैं भौतिक वियोजन (अर्थात् “एन्क्लेव” के निर्माण) और व्यावसायिक वियोजन (अर्थात् लैंगिक सरोकारों से संबद्ध कार्य ही असंगत रूप में महिला अधिकारियों को सौंपने) के दुष्परिणामों पर आगे की छानबीन करने के लिए उत्तर भारत के अनेक राज्यों के पुलिस थानों के संबंध में नृवंशविज्ञान पर आधारित शोधकार्य कर रहा हूँ. मुझे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित संस्थाओं में शिकायतकर्ताओं को खुलकर बोलने की गुंजाइश रहती है और ऐसे निकायों में “परामर्श” से न्याय करने की अनौपचारिक प्रणाली रहती है. साथ ही लैंगिक हिंसा के शिकार पीड़ितों को उन पर अत्याचार करने वाले अपराधियों के साथ मेल-मिलाप करने के लिए कहा जा सकता है. दूसरे शब्दों में, कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों की “न्याय पाने की” अपनी ही परिभाषा होती है और लैंगिक पहचान पर आधारित प्रशासकों के मात्र वियोजन से आपराधिक न्याय प्रणाली के परिणामों में औपचारिक तौर पर भारी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता.
तीसरे अध्ययन के दौरान अपने सहलेखक शैरों बर्नहार्ट्ड के साथ मैंने परीक्षण किया कि क्या (व्यावसायिक) वियोजन का असर कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों के भरोसे पर अधिक पड़ता है. वियोजन के रूप में प्रतिनिधित्व के पीछे एक महत्वपूर्ण धारणा तो यही है कि महिलाएँ खास तौर पर लैंगिक मामलों को सुलझाते समय सामूहिक प्रशासकों पर अधिक भरोसा करती हैं.
इंडियाज़ न्यूज़ कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली टेलीविज़न से संबद्ध वृत्तचित्रों के साथ किये गए वीडियो-आधारित प्रयोग की मदद से हमने यह दर्शाया है कि खास तौर पर अन्य महिलाओं द्वारा की गई लैंगिक शिकायतों का निवारण करते हुए महिला पुलिसकर्मी कम पक्षपात करती दिखाई पड़ती हैं. खास तौर पर महाराष्ट्र राज्य में 1,000 से अधिक उत्तरदाताओं के प्रतिनिधि नमूनों को उन तमाम समाचार बुलेटिनों में हेरफेर के साथ दिखाया गया है जिनमें जाँचकर्ता अधिकारी की लैंगिक सूचना और उस केस के प्रकार में रद्दोबदल की गई थी. उदाहरण के लिए, जब कभी महिला उत्तरदाता किसी महिला पुलिसकर्मी को दहेज के मामले की जाँच करते हुए देखती थीं तो संभावना इस बात की रहती थी कि वे उस अधिकारी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते समय पुरुष पुलिसकर्मी की तुलना में उसे कम करके आँकती थीं. जाँच-परिणामों से पता चलता है कि साझा लैंगिक पहचान के कारण और उन तमाम समूह-विशिष्ट निकायों के कारण जिनमें समान पहचान के आधार पर उन्हें कार्य सौंपे गए हैं, जन अधिकारियों के प्रति भरोसा अपने-आप नहीं बढ़ सकता.
काल्पनिक योगदान के अलावा कुछ नीतिगत निहितार्थ तो लागू हो ही जाएँगे. नीतिगत संरचना और मौजूदा सांस्कृतिक प्रतिमानों और नौकरशाही के ढाँचों के बीच परस्पर अंतः क्रिया तो अप्रत्याशित रूप में हो सकती है, लेकिन नीति को लागू करते समय इन प्रतिमानों और संरचनाओं का भी ध्यान रखना होगा. उदाहरण के लिए अगर समूह-विशिष्ट निकायों की संरचना वैकल्पिक संसाधन के रूप में की जाए तो शिकायतकर्ताओं के मामलों को फिर भी आगे ढकेला जा सकता है और तब भी यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि निकायों की संरचना से वहाँ तक पहुँचने के मार्गों का विस्तार होता है या फिर ये मार्ग संकुचित हो जाते हैं. इसके अलावा, राज्य की कमज़ोर क्षमता के कारण कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ेगा और स्टाफ़ की कमी भी रहेगी; इन चुनौतियों का सामना करते समय कुछ पुलिस अधिकारी कुछ हद तक तो यौन हिंसा के मामलों को गंभीरता से लेने में सफल भी हो जाएँगे. फिर भी इस बात की संभावना हमेशा ही बनी रहेगी कि अल्पसंख्यक समूहों के प्रशासक पक्षपात से मुक्त नहीं रह पाएँगे, क्योंकि यह भावना पुलिस की उप-संस्कृति में व्यापक तौर पर निहित है और ऐसी स्थिति में कुछ मुद्दे अन्य मुद्दों की तुलना में तरजीह पा लेंगे. जहाँ तक उनके रवैय्ये और प्रतिमानों में बदलाव लाने की बात है, यह तो लैंगिक संवेदना को बढ़ाकर और प्रशिक्षण के अन्य तरीकों की मदद से ही किया जा सकता है. अंततः वियोजित प्रतिनिधित्व को दृढ़ता से लागू करने पर भी कोटे की तरह समावेशी संरचना को लागू नहीं किया जा सकता. पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों के बिना एन्क्लेवों की स्थापना से संस्थाओं के समंदर में अनेक द्वीप बन जाएँगे और उन पर बहुसंख्यक पुलिसकर्मियों का वर्चस्व बना रहेगा और पुरुष और महिला प्रशासकों के बीच अंतः सामूहिक संवाद घटता जाएगा. सभी प्रकार के मामलों (लैंगिक और गैर-लैंगिक मामलों) को निपटाने के लिए समूह-विशिष्ट निकायों को सक्षम बनाने के अलावा मौजूदा पुलिस थानों में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती से भौतिक और व्यावसायिक वियोजन को कम किया जा सकता है.
निर्विकार जस्सल स्टैनफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के किंग वैश्विक विकास केंद्र में पोस्ट डॉक्टरल फ़ैलो हैं.
हिंदी अनुवादः डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@gmail.com> / मोबाइल : 91+9910029919