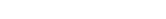मणिपुर में भारतीय सैन्यबल पर घात लगाकर किये गये हमले, नागालैंड में एनएससीएन-आईएम के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर और गुरदासपुर हमले के कारण आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नरेंद्र मोदी के एजेंडे में केंद्र पर आ गया है.सशस्त्र गुटों के साथ संघर्ष करने का भारत का अपना लंबा इतिहास है, फिर भले ही ये नक्सलवादी हों, आदिवासी अलगाववादी हों या कश्मीरी लड़ाके हों. फिर भी भारत ने इन सशस्त्र गुटों के साथ संघर्ष करते हुए जो अनुभव हासिल किया है, उसकी इन सशस्त्र गुटों से निपटने में लोकप्रिय और नीतिगत बयानों में लगातार अनदेखी की जाती रही है. संघर्षों के इस लंबे इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिल सकती थी, लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया.
सबसे पहली बात तो यह है कि युद्ध क्षेत्र में “विकास” का मतलब सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले आम तौर पर कहीं अधिक जटिल होता है. युद्ध क्षेत्र में हिंसा के वातावरण में आर्थिक विकास और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में केंद्रीय निधि उपलब्ध कराने की लुभावने शब्दों में बात करना तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों में संलग्न लोगों को इसमें एक विकल्प दिखाई देता है, लेकिन विकास राशि तभी कारगर हो सकती है जब उसका इस्तेमाल सोच-समझकर सही ढंग से किया जाए और उस पर निगरानी रखी जाए, लेकिन इस सीधी-सादी नीति के परिणाम अक्सर कुछ नहीं निकलते. सशस्त्र गुटों के कई नेता बेरोज़गार और अशिक्षित युवा नहीं होते, बल्कि वे सम्मानित मध्यवर्ग के शिक्षित बालक होते हैं. इस बात की पूरी संभावना है कि काम करते हुए और शिक्षा ग्रहण करते हुए भी वे राजनैतिक यथास्थिति से अप्रभावित ही रहे हों. विकास की पहल से इनमें से कुछ रंगरूट और समर्थक तो हिंसक गतिविधियों से अपने-आपको अलग कर सकते हैं, अनेक गरीब इलाके ऐसे भी हैं जहाँ विद्रोह के स्वर नहीं उठते और अधिकांश विद्रोही भी गरीब नहीं होते. गरीबी और विद्रोह के बीच गहरे संबंधों की कल्पना करके भी किसी सुसंगत नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता.
विकास निधि भी उस समय उलटी पड़ सकती है, जब उसका उचित वितरण नहीं होता और यह बहुत आम बात है. केंद्रीय निधि को अक्सर स्थानीय राजनीतिज्ञ, उनके परिवार और उनके संरक्षण में पलने वाले भाई-बंधु ही चट कर जाते हैं. इससे भ्रष्टाचार फलता-फूलता है, ज़िम्मेदारी की भावना कम हो जाती है और नौकरशाही का असर भी घटने लगता है. कश्मीर में सरकार से जुड़े अनेक घोटालों के खुलने से यह बात तो साफ़ हो गई है कि जब स्थानीय पावर ब्रोकर और मज़बूत हो जाते हैं तो क्या होता है और वे “भारत समर्थक” और “मुख्य धारा” के अपने राजनीतिज्ञों के भले के लिए भी अपने मातहत लोगों से कुछ नहीं करवा पाते. इससे अंततः भारत के व्यापक हितों को बल ज़रूर मिलता है, जैसा कि ए.एस. दौलत के हाल ही में कश्मीर में पैसे के उपयोग से संबंधित रहस्योद्घाटन से पता चला है, लेकिन व्यापक समृद्धि को लाने का तरीका इससे बिलकुल अलग है.
यह पैसा उग्रवादियों के हाथ में भी जा सकता है. वे लोग नौकरशाहों और कल-कारखानों से सीधे ही पैसे वसूलते हैं और सशस्त्र गुटों से जुड़ी या उनके द्वारा स्वाधिकृत कंपनियाँ सरकार से ठेके प्राप्त करती हैं. नागालैंड इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि किस प्रकार सरकारी पैसा सैन्यबलों के पास पहुँचने के बजाय सशस्त्र गुटों के पास पहुँच जाता है. आंतरिक सुरक्षा नीति में संसाधन उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह इतना भी सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जटिल राजनैतिक पहल का निष्प्रभावी विकल्प है.
दूसरी बात यह है कि सरकारी मार्ग भी अलग-अलग तरह के होते हैं. कुछ मामलों में, जैसे अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में और नब्बे के दशक के आरंभ में पंजाब में, सत्तर के दशक के आरंभ/मध्य में बंगाल में और नब्बे के दशक में कश्मीर में सरकारी तरीके बहुत आक्रामक और अक्सर क्रूर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों ने अपने ऑपरेशन से आतंकी वारदातों को खत्म कर दिया. इन सरकारी अभियानों में मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ा दी गईं. लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने और “मानवीय स्पर्श” के लुभावने शब्दों के बावजूद ये कार्रवाइयाँ घटिया और निष्ठुर रहीं. भारतीय सेना और गृह मंत्रालय ने इन युद्ध क्षेत्रों (आतंकी गतिविधियों से ग्रस्त क्षेत्रों) में हुई वारदातों के लिए संयत भाषा का ही प्रयोग किया है, लेकिन हम इनकी वास्तविकताओं को भी झुठला नहीं सकते.
परंतु दूसरे मामलों में, खास तौर पर अस्सी के दशक में मिज़ोरम में सशस्त्र गुट के साथ सीधी वार्ताएँ की गईँ, जिनके फलस्वरूप शांति समझौते किये गये और उन्हें अपने राजनैतिक ढाँचे में शामिल कर लिया गया. अगर व्यापक आधार पर सशस्त्र गुट के साथ बातचीत की जाए तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है. इन समझौतों की सफलता तभी संभव होती है जब हम स्थानीय लोगों को उसमें शामिल करें और उन्हें वहाँ बसने का लाभ मिलने लगे और इन समझौतों के कार्यान्वयन में “रोड़ा अटकाने वाले तत्वों” को ऐसा करने से रोका जाए.
पिछले दो दशकों में नागालैंड में और उत्तरी मणिपुर के कुकी इलाकों में कितनी ही युद्धविराम और समझौता-वार्ताएँ होते देखी हैं, जिनके कारण वहाँ पर न तो एकतरफ़ा सरकारी हिंसा हुई और न ही व्यापक हिंसा की वारदातें हो पाईं. इन क्षेत्रों में राज्य और सशस्त्र गुटों के बीच सीमित सहयोग ही रहा, जिसके कारण कभी-कभी हिंसक झड़पें हो जाती हैं, लेकिन ये झड़पें स्थायी भी हो सकती हैं. वस्तुतः सरकारी वर्चस्व बनाये रखना भी हिंसक झड़पों को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है.
राज्य के लिए कोई एक ऐसा उपाय नहीं है, जो “कारगर” हो सकता हो. राजनैतिक पंडित और सुरक्षा प्रबंधक ऐसी झड़पों को रोकने के लिए अलग-अलग मौलिक अपनाते रहे हैं. इन उपायों में उन्हें बलपूर्वक दबाने का उपाय भी होता है और जियो-और जीने-दो की सौदेबाजी भी शामिल रहती है. किसी एक सिद्धांत या समाधान की रणनीति अपनाने के बजाय बहुत-सी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, उनमें से कुछ रचनात्मक होती हैं और कुछ प्रयोगधर्मा.
तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की विश्वासघाती गतिविधियों से बचने के लिए स्थानीय गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं हैं. इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने हिंसक झड़पों को बढ़ावा देने के लिए विध्वंसक भूमिका अपना रखी है. खतरनाक और उग्रवादी सशस्त्र गुटों पर निर्भर रहने के लिए उनकी सेना की भर्त्सना की जानी चाहिए. स्थानीय परिस्थितियों से बेपरवाह पाकिस्तान की कट्टरवादी नीति के कारण ही खास तौर पर कश्मीर में असंतोष का वातावरण अक्सर बना रहता है.
पाकिस्तानी नीति की खासियत ही यही है कि उसे ज़मीन से जुड़े लोगों की कोई परवाह नहीं होती. उनकी रणनीति ही यही होती है कि एक मकसद तय करके भय का वातावरण बनाया जाए, भले ही भारत में मुख्यधारा के लोगों की भावनाएँ इससे आहत होती हों. कठिन सवालों से बचने के लिए ही पाकिस्तान यह उलझन बनाये रखता है. इस नीति के कारण वह राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाये रखना चाहता है. इसके बावजूद भी भारत के नीति-निर्माताओं और जनता को चाहिए कि वे कश्मीरियों की भावनाओं की ख्याल रखें.
अंततः राजनीति को जन-संबंधों, वित्तीय अंतरण या चुनाव में भारी संख्या में भाग लेने से जोड़कर नहीं देखा जा सकता.भारत की सीमाओं के अंदर, खास तौर पर अस्थिर इलाकों में रहने वाले बहुत से लोग अपने –आपको भारतीय भी नहीं मानते या फिर यह मानते हैं कि वे साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल में फँसे विरोधी राज्य में रहते हैं. “सामान्य स्थिति” बहाल करने की बात करना भी कश्मीर और नागालैंड जैसे राज्यों के गहन इतिहास को झुठलाने की कोशिश करना है. संघर्ष के इन क्षेत्रों को भारत की सर्वसमावेशी छवि में शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि वास्तविक कल्पना के आधार पर निर्भीकता के साथ जोखिम उठाया जाए ताकि सतत समावेशी राजनैतिक व्यवस्था कायम की जा सके. इसके लिए ज़रूरी है कि शीर्षस्थ नेतृत्व के माध्यम से राजनैतिक प्रयास किये जाएँ. इसके बिना रोज़मर्रे की नीतियों की कमान नौकरशाही, सैन्य अधिकारियों और स्थानीय पदाधिकारियों के हाथों में ही बनी रहती है और वे यथास्थिति को बदलने के लिए कोई भी मौलिक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते.
दक्षिणपंथियों के बीच अपनी विश्वसनीयता और अपने राजनैतिक कौशल के कारण प्रधानमंत्री मोदी बड़े-बड़े सुधार लाने में खास तौर पर पूरी तरह से सुसज्जित रहते हैं. पूर्वोत्तर में एनएससीएन-आईएम के साथ हाल ही के समझौते के कारण नागालैंड का दशकों पुराना संघर्ष समाप्त करने में मदद मिल सकती है. नागालैंड और पूर्वोत्तर में किये गये पिछले समझौतों की दशा से बचने के लिए आवश्यकता इस बात है कि नगा लोगों को व्यापक समावेशी समझौते में शामिल किया जाए. बहुत-से समझौते तो हस्ताक्षर होने के एकदम बाद ही विफल हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए. हालाँकि मणिपुर में हाल ही में हुई मुठभेड़ से निपटने के लिए जिस दक्षता से सैनिक अभियान चलाया गया, उसकी प्रैस में काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन वास्तविक समाधान तो तभी होगा जब मणिपुर के अंदर ऐसा कोई राजनैतिक समाधान किया जाए जिससे असंतुष्ट विद्रोहियों को राजनैतिक दृष्टि से संतुष्ट किया जा सके, स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जा सके और उन तमाम निर्गुट राजनीतिज्ञों को सशक्त किया जा सके जो दिल्ली के अनुदान पर निर्भर नहीं रहते. बस इसका विकल्प यही रहेगा कि विद्राहियों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय और सैन्य बलों द्वारा पिछले तीन दशकों से चलाया जा रहा ऑपरेशन आगे भी इसी तरह धीरे-धीरे घिसटता रहे. पूरे क्षेत्र में विकास के लिए दी जाने वाली सहायता-राशि का सही लक्ष्य होना चाहिए और ऐसे शांति समझौते किये जाने चाहिए जिनसे निहत्थे नागरिकों और सशस्त्र गुटों को साथ लाने में मदद मिलती हो.
जम्मू व कश्मीर मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी. वह अपने हिंदू राष्ट्रीय लोगों की कठोर प्राथमिकताओं को आगे भी जारी तो रख सकते हैं, लेकिन इससे राज्य में स्थायी तौर पर सुधार नहीं लाया जा सकता. भले ही बहुत नाटकीय मोड़ की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे पिछले दो दशकों से लंबित अनेक उपेक्षित आयोगों और वार्ताकारों की रिपोर्टों में की गई कुछ सिफ़ारिशों को लागू किया जा सके ताकि कश्मीर की घाटी में बड़े राजनैतिक गुटों को फिर से सिर उठाने और स्थिति का लाभ उठाने और राज्य में तैनात सुरक्षा बलों से जवाबदेही माँगने का मौका न मिल सके. इन सिफ़ारिशों में एक है, अफ़्स्पा (AFSPA ) की गंभीरता से समीक्षा की जाए, क्योंकि इसी के कारण स्थानीय भावनाओं को सबसे पहले भड़कने का मौका मिलता है. इस तरह की पहल से एक ठोस कार्रवाई की शुरुआत हो सकेगी और अकर्मण्य राजनीति के रूप में जो यथास्थिति बनी हुई है, उस गतिरोध को खत्म करने में मदद भी मिलेगी. मोदी ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की बात की है, लेकिन अग्नि-परीक्षा तो तब होगी जब दिल्ली और उससे संबद्ध ताकतों के बीच नये सिरे से संबंधों में स्थायी सुधार होगा.
पॉल स्टेनलैंड शिकागो विश्वविद्यालय में राजनैतिक विज्ञान के सहायक प्रोफ़ेसर हैं.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@gmail.com> / मोबाइल : 91+9910029919.