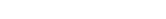सन् 2018 में कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गाँधी ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए 2014 के चुनाव में अपनी पार्टी की पराजय के कारणों को गिनाया था. अन्य कारणों के अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि “भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है.” इस भाषण से यह स्पष्ट हो गया था कि ए.के. एंथॉनी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेतृत्व ने ए.के. एंथॉनी के इस विश्लेषण को पहली बार स्वीकार किया था कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार का कारण यह धारणा थी कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में विश्वास करती है.
निश्चय ही कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी नहीं थी, जो “मुस्लिम पक्षपात” की धारणा को साफ़ तौर पर दुरुस्त करने में जुटी हुई थी. खास तौर पर उत्तर भारत की कई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ अंदर ही अंदर यह सोच रही थीं कि मौजूदा राजनीतिक संस्कृति में उनके राजनीतिक मंच पर मुस्लिम या “मुस्लिम सोच” की स्पष्ट उपस्थिति घातक सिद्ध हो सकती है.
परंतु, धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ अभी-भी यह कल्पना करती हैं कि मुसलमानों का समुदाय एक ऐसा समरूप समुदाय है जिसके साथ उनके राजनीतिक हित साफ़ तौर पर जुड़े हुए हैं और मुस्लिम “वोट-बैंक” संबंधी अपने इस दावे को वे किसी भी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. तथापि भारतीय जनता पार्टी के मज़ूबत सिस्टम ने इन पार्टियों के अपने मुस्लिम मतदाताओं से जुड़े रिश्तों के पैटर्न को झकझोर कर रख दिया है.
असंबद्ध परिवर्तनः मुस्लिम मुद्दों की राजनीति
धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ मुसलमानों को जुटाने के लिए मुस्लिम मुद्दों के परंपरागत पैकेज से अलग हट गई हैं. जैसा कि हिलाल अहमद ने अपनी पुस्तक Siyasi Muslims में तर्क देते हुए लिखा है कि मुस्लिम वोट-बैंक की कल्पना मुस्लिम मुद्दों के खास ढाँचे पर ही आधारित थी. ये मुद्दे थे, बाबरी मस्जिद, पर्सनल लॉ, उर्दू और जामिया विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय. धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और मुस्लिम नेताओं ने इस समुदाय के वोट हासिल करने के लिए इन मुस्लिम मुद्दों को ही प्रमुख साधन बना रखा था.
इन सभी मुद्दों में एक साझा डिनॉमिनेटर हैः ये सभी मूलतः “नकारात्मक मुद्दे” हैं, जिनका संबंध मुसलमानों के लिए कुछ मौजूदा “विशेषाधिकारों” के संरक्षण से है. भले ही ये सभी मुद्दे (पर्सनल लॉ, बाबरी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) आदि हिंदू बहुसंख्यक विमर्श के मुख्य बिंदु हैं, फिर भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ इन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से अपनी राय बना लेती हैं. “हिंदुओं के एकजुट होने” के भय के कारण ही ये पार्टियाँ “मुस्लिम मुद्दों” से असंबद्ध रूप में दूर होती जा रही हैं.
तीन तलाक बिल और राम मंदिर संबंधी निर्णय को भी निष्क्रिय रहते हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया गया. इसलिए मुसलमानों के कुछ नीतिगत प्राथमिक मुद्दों (पर्सनल लॉ, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) आदि) के संरक्षण का दावा करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ अब आम तौर पर मुसलमानों के संरक्षण की बात करने लगी हैं.
भाजपा की इस अपरिभाषित चुनौती से मुकाबला करने के लिए मुस्लिम समुदाय से सामूहिक रूप में वोट देने की प्रार्थना की जाने लगी है. जिन राज्यों में मुसलमानों के अनेक गैर-भाजपा विकल्प हैं, वहाँ ये पार्टियाँ अपने-आप में एक दूसरे से होड़ करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि उनकी पार्टी ही भाजपा की धुर विरोधी पार्टी है.जब भगवा पार्टी की मुख्य विरोधी पार्टी पर मुसलमानों के वोट काटने का आरोप लगाया जाता है तो उसे “भाजपा की B टीम” कह दिया जाता है और उसे “B टीम” कहकर प्रचारित किया जाता है. ऑल इंडिया मजलिस-ए- मुसलमीन (AIMIM), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और जनता दल (सेक्युलर) (JD[S]) जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को हाल ही में “B ‘टीम” कहा जाने लगा था. इसलिए “मुस्लिम वोट बैंक” का असली मकसद भाजपा को हराना ही होता है.
दूसरी बात यह है कि मुस्लिम सशक्तीकरण के असंबद्ध अंतराल को भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने मुस्लिम पहचान पर केंद्रित पार्टियों के लिए कम कर दिया है. सच्चर समिति के बाद के चरण में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के मामले में,खास तौर पर अल्पसंख्यकों के कोटे के संदर्भ में अधिक दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था. उदाहरण के लिए, 2012 के उ.प्र. के 2012 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी-दोनों ने ही नौकरियों में अल्पसंख्यकों के आरक्षण की माँग उठानी शुरू कर दी थी. मुसलमानों के “आर्थिक पिछड़ेपन” की चर्चा बहुत होती है और यू.पी.ए. सरकारों के अंतर्गत इस पर किये गए अध्ययन से इसकी पुष्टि भी हो गई थी. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने वामपंथियों पर इसके आधार पर ही हमला किया था. इसके एक दशक के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में अगर किसी एक पार्टी ने मुसलमानों के “पिछड़ेपन” के विमर्श को चुनावी मुद्दा बनाया तो वह पार्टी थी, AIMIM. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने “सुरक्षा की राजनीति” पर बल देते हुए मुसलमानों को आगाह किया कि इंडियन सैक्युलर फ़्रंट (ISF) के अब्बास सिद्दीकी ने “मुसलमानों के वोटों को बाँटने के लिए भाजपा से पैसे लिये हैं ...और अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो मुसलमानों पर सबसे बड़ा खतरा मँडराने लगेगा.”
इसी बीच इंडियन सैक्युलर फ़्रंट (ISF) ने (धार्मिक नारों के अलावा) तृणमूल कांग्रेस के मुसलमानों के साथ रिश्ते को “धोखा” करार देते हुए “आर्थिक पिछड़ेपन” की शब्दावली का उपयोग किया था.
धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए मतदाताओं के बीच हिंदू बहुसंख्यावाद के प्रचार के कारण मुसलमानों की पहचान और मुस्लिम सशक्तीकरण के हालिया मुद्दे जैसे परंपरावादी मुद्दों को भुनाने की बहुत कम गुंजाइश ही बची थी. जहाँ एक ओर सुरक्षा की राजनीति से भाजपा की मुख्य विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में और राष्ट्रीय जनता दल (RJD)-कांग्रेस के गठबंधन को बिहार में मुसलमानों के तीन-चौथाई वोट मिलने में मदद मिली, वहीं यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस रणनीति की दीर्घकालीन विश्वसनीयता कितनी है. वस्तुतः बिहार के सीमांचल क्षेत्र में या निचले असम और बराक घाटी पर ऑल इंडिया युनाइटेड डैमोक्रेटिक फ़्रंट (AIUDF) की पकड़ बने रहने से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वहीं पर संघर्ष करती हैं जहाँ आकांक्षाओं की राजनीति सुरक्षा की राजनीति पर भारी पड़ती है.
कार्यमूलक परिवर्तनः प्रतिनिधित्व की राजनीति
मुस्लिम मुद्दों के असंबद्ध परिवर्तन के साथ-साथ,धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर भी विचार करना शुरू कर दिया है. चूँकि “मुस्लिम मुद्दे” चुनावी दृष्टि से मुसलमानों को जुटाने के लिए अब मुख्य धुरी के रूप में कारगर नहीं होते, इसलिए मुसलमानों के इन मुद्दों का लाभ उठाने में मुस्लिम धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की कार्यमूलक उपयोगिता में तदनुरूपी गिरावट आ रही है. धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ अब इन मुस्लिम बिचौलियों पर कम निर्भर रहती हैं और मुस्लिम मतदाताओं से सीधे संपर्क बनाने की कोशिश में जुट गई हैं.
कई अध्ययनों से पता चलता है कि चुनावी मैदान में मुस्लिम धार्मिक नेताओं की प्रासंगिकता बहुत समय से घटने लगी है. धर्मनिरपेक्ष ढंग से मध्यम वर्ग के छात्रों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा चलाये गए नागरिकता संशोधन (CAA) विरोधी बिल के आंदोलन के कारण मुसलमानों के बीच उलेमाओं का जो बचा-खुचा राजनीतिक प्रभाव था,वह भी खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश के हाल ही के चुनावों में मुल्लाओं का थोड़ा-बहुत प्रभाव भी दिखाई नहीं पड़ा. वास्तव में अगर किसी एक पार्टी ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किया तो वह है उत्तर प्रदेश कांग्रेस,जिसने इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के मियाँ तौकीर रज़ा के साथ मिलकर इसके लिए प्रयास किया और भारी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर इसे ठुकरा दिया. इसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-वामपंथियों के साथ गठबंधन करने वाले तेज़-तर्रार मुल्ला अब्बास सिद्दीकी को मुसलमानों के बहुत कम वोट मिल पाए. यह उल्लेखनीय है कि अब केवल वही पार्टियाँ धार्मिक नेताओं की मदद लेती हैं जो चुनावी दौड़ में तीसरे या चौथे नंबर पर रहती हैं और अंतिम प्रयास के रूप में मुसलमानों को रिझाने का प्रयास करती हैं जबकि पिछले ज़माने में यही रणनीति सबसे अधिक कारगर मानी जाती थी.
इसी तरह धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ मुस्लिम चेहरों को तरजीह देने में भी पीछे रहने लगी हैं. यह सच है कि ऐतिहासिक रूप में मुस्लिम सांसद और विधायक धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की नीति के अनुरूप ही चलते रहे हैं और वे अपनी अलग आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं करते हैं. लेकिन ये पार्टियाँ केवल उन मुस्लिम चेहरों को ही महत्व देती हैं जिनका राज्य-स्तर / देशव्यापी स्तर पर कोई प्रभाव होता है और जो “मुस्लिम मुद्दों” को पार्टी की नीति के अनुरूप दृढ़ता से उठाते हैं (जैसे,समाजवादी पार्टी में आज़म खान, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में अशरफ़ फ़ातमी और कांग्रेस में सलमान खुर्शीद ). ऐसे प्रतीकात्मक चेहरों की आवश्यकता अब नहीं रही.. समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिना किसी प्रमुख मुस्लिम चेहरे को सामने रखते हुए चुनाव प्रचार किया और इसके बावजूद भी भारी संख्या में मुस्लिम वोट प्राप्त करने में कामयाब हुए. वस्तुतः समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव से पहले दो वर्षों तक कानूनी पेच में फँसे हुए आज़म खान से बड़ी होशियारी के साथ दूरी बनाये रखी. धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधियों ने कर्तव्य भावना के साथ पार्टी की नीतियों का अनुसरण किया और उन तमाम मुद्दों पर चुप्पी बनाये रखी जिनसे उनकी पार्टी के “ध्रुवीकरण” की संभावना हो सकती थी. इसके अलावा, मुसलमानों को भी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में बहुत कम देखा जाता है. उत्तर प्रदेश में बसपा ने बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा,लेकिन उनमें से कोई भी (उनके 403 प्रत्याशियों में से 91) चुनाव नहीं जीत पाया. धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ बिना किसी स्पष्ट मुस्लिम चेहरे के भी मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के साथ सीधे ही संपर्क बनाने में जुट गई हैं ताकि वे भाजपा के “मुस्लिम तुष्टीकरण ” के मुख्य आरोप का जवाब दे सकें.
राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों को फिर से परिभाषित करना
यह बात तो माननी होगी कि राज्यों के अनुसार विश्लेषण करने पर यह मुद्दा और भी जटिल हो जाता है. मुसलमानों के प्रति धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की स्थिति संबंधित राज्यों में राजनीतिक होड़ पर भी निर्भर करती है -भले ही वहाँ उनकी पार्टी द्विकोणीय मुकाबले में फँसी हो या बहुकोणीय मुकाबले में. उदाहरण के लिए, तेलंगाना में कांग्रेस के मुखिया रेवंत रेड्डी ने ज़ोर देकर कहा कि मुसलमान दलितों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) की सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है. कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व ने, खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने स्कूल में हिजाब पर लगी पाबंदी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. मुस्लिम सशक्तीकरण और मुसलमानों की पहचान से संबंधित ऐसे विमर्श को उस राज्य की कांग्रेस इकाई द्वारा राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ उनका सीधा मुकाबला भाजपा से है, अपनाना बहुत कठिन होगा. इसी प्रकार समाजवादी पार्टी (SP),राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए अपने राज्यों में चलने वाली राजनीतिक होड़ में बढ़ते द्विकोणीय मुकाबले के कारण अपने रुख में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है और यही कारण है कि भाजपा की स्थिति वहाँ मजबूत होती चली जाती है.
पार्टी के अंदर रचनात्मक अंतर्विरोध को लिए भी कुछ गुंजाइश बनी रहती है. उदाहरण के लिए कांग्रेस के अंदर “मुस्लिम मुद्दों” से असंबद्ध दूरी बनाने के कारण बंगाल में ISF और असम में AIUDF जैसी मुस्लिम पहचान पर केंद्रित पार्टियों के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई गई. इन अस्पष्टताओं के कारण पार्टी में बहस भी छिड़ गई थी. पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने ऐसे गठबंधनों की आलोचना की थी और इस बात पर बल दिया था कि “अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता-दोनों ही समान रूप से देश के लिए घातक हैं.” इसकी प्रतिक्रिया में सलमान खुर्शीद ने पार्टी के रुख का बचाव करते हुए नेहरू की चेतावनी को उद्धृत किया कि “बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता से कहीं अधिक खतरनाक है.”
भाजपा का मज़बूत सिस्टम उभरने के कारण मुसलमानों के प्रति धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के रुख की कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आ गईं, मुसलमानों की पहचान की बात अब पुरानी पड़ गई है और मुस्लिम वोट-बैंक में शोषण की भावना निहित रही है. धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की प्रतिक्रिया मुसलमानों की उपस्थिति या उनके राजनीतिक मंचों पर "मुसलमानियत" को कम करने की रही है. हालाँकि, वे मुसलमानों की चुनावी लामबंदी में "संरक्षण की राजनीति" के प्रमुख रुख पर अड़े हुए हैं, जबकि संरक्षण की शब्दावली में भी अब भारी बदलाव आ गया है. बस यही आशा की सकती है कि मौजूदा चरण संक्रमण की अवधि है और धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ इससे पहले ही अपनी मुस्लिम कल्पना को फिर से अधिक रचनात्मक स्वरूप दे पाएँगी.
आसिम अली एक स्वतंत्र राजनीतिक शोधकर्ता हैं.
हिंदी अनुवादः डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (हिंदी), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@gmail.com> / Mobile : 91+991002991/WhatsApp:+91 83680 68365