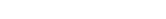पहचान की राजनीति करना भारत के मानवीय संवाद के अधिकांश विश्लेषण का सबसे अधिक उपयोगी काम रह गया है. कई दशकों तक तो जाति और समुदाय की खाई को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जाता था, क्योंकि इसीसे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक गतिशीलता के स्वरूप को आकार मिलता था. जिस हद तक लोग व्यक्तिगत स्तर पर हिंसक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, सामूहिक तौर पर हिंसक हो जाते हैं, सार्वजनिक हितकारी कामों को सफलता से पूरा करते हैं या चुनाव के दिन निर्णय लेते हैं – सभी कुछ जातीय पहचान के दायरे में देखा जाता है.
फिर भी इन तमाम प्रकार के विश्लेषणों में एक ही धारणा को बल मिलता है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाताः कि लोग व्यक्तिगत रूप में आसानी से और सही तौर पर दूसरों की जातीय पहचान को चिह्नित कर लेते हैं. समाज विज्ञान की शब्दावली में यही “जातीय पहचान की क्षमता” की धारणा है. सच तो यह है कि दुनिया-भर से प्राप्त और अधिकाधिक बढ़ते साक्ष्य से इस धारणा पर भी संदेह होने लगा है. इस साक्ष्य में भारत में हाल ही में हुई शोध भी शामिल है. खास तौर पर चुनावी वर्ष में जब चारों ओर “वोट बैंक” और “जातीय समीकरण” की चर्चा होती है तो हमें ठिठक कर एक ही सवाल करना चाहिए, कहीं हम जाति को अधिक महत्व तो नहीं दे रहे हैं?
जातीय लगाव को भारत में उम्मीदवारों के मूल्यांकन और मतदाताओं की अपेक्षाओं को आकार देने और निश्चय ही मतदाता की पसंद पर निर्णायक फैसला देने जैसे कई रूपों में व्यापक तौर पर मतदान के स्वरूप को प्रभावित करने वाला एक उपाय माना जाता है. उदाहरण के लिए, ऐसे सभी बयानों में सबसे अधिक दबी ज़बान में एक बयान होता है, ब्राह्मणों के बारे में .. यह तय करना कि उम्मीदवार ब्राह्मण, यादव या मुसलमान है. बल्कि इस मूलभूत धारणा से तो मतदाताओं के दिमाग में सभी प्रकार की गणनाएँ होने लगती हैं.
यह धारणा कितनी वास्तविक है? विकासशील समाजों के दिल्ली स्थित अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) की मदद से हमने यह परीक्षण बिहार के यादृच्छिक रूप में चुने हुए चालीस चुनाव क्षेत्रों के 2,000 मतदाताओं के सामने रखा. सन् 2010 के विधान सभा के चुनाव में डाले गये मतदान (जिसमें नीतीश कुमार जीतकर सत्ता में आये थे) के कुछ दिन के बाद ही हमने मतदाताओं से हाल ही के विधान सभा के चुनाव में उनके द्वारा जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया था, उसकी जाति के बारे में पूछा. मतदाताओं की प्रतिक्रियाओं का हमने उम्मीदवारों की वास्तविक पहचान के डेटा से मिलान किया. बिहार ऐसे परीक्षण के लिए एक अच्छी जगह थी. सारे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जातिगत विभाजन इतना स्पष्ट हो और रोज़मर्रे के जीवन पर उसका सबसे अधिक असर भी दिखायी भी देता हो.
हमारे लिए कुछ हद तक यह भी विस्मय की बात थी कि बिहार में हमारे द्वारा सर्वेक्षण किये गये लगभग एक तिहाई मतदाताओं (29.2 प्रतिशत) ने कुछ दिन पहले ही किये गये मतदान में उम्मीदवारों की जाति की गलत पहचान की थी. इसका असर सन् 2010 में इंडियन बिज़नेस स्कूल (आईबीएस) के छात्रों के सहयोग से ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों पर भी पड़ा. न केवल आईबीएस के अधिकांश छात्र अपने साथी सहपाठियों के जाति वर्ग को पहचानने के लिए जी-जान से कोशिश में जुट गये थे बल्कि अधिकांश विषयों के छात्र भी अन्य जाति वर्ग की पहचान बनाने में सफल हो गये थे.
वास्तविकता तो यह है कि जब बिहार के मतदाताओं ने इसे गलत सिद्ध कर दिया तो अधिकांश मामलों में भी वे बहुत गलत भी नहीं थे. जहाँ एक ओर लगभग एक तिहाई प्रतिभागियों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार की जाति को पहचानने में गलती की, वहीं लगभग 90 प्रतिभागियों ने उम्मीदवार की मानी हुई जाति को अपने ही व्यापक जाति वर्ग में स्वीकार कर लिया. उदाहरण के लिए, हो सकता है कि मतदाता ने भूमिहार की उच्च जाति को पहचानने में गलती की हो, और वस्तुतः उम्मीदवार उच्च ब्राह्मण जाति का हो. जब कोई मतदाता अपने उम्मीदवार की जाति को पहचान नहीं पाता तो वह आम तौर पर अनुमान से ही काम ले रहा होता / होती है.
थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इससे कोई बात साफ़ नहीं होती. अंततः यह जातिगत पहचान ही है जो बिहार और भारत के अन्य भागों में आम तौर पर स्पष्ट विभाजन रेखा समझी जाती है और यह बात व्यापक वर्गों ( अनुसूचित जाति, उच्च जाति, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) आदि) से संबंधित नहीं है.
वस्तुतः जब भी कोई यात्री चुनाव के दिनों में किसी चुनाव क्षेत्र का दौरा करता है तो स्थानीय लोगों से पहले-पहल उसे दो तरह की सूचनाएँ मिलती हैं. एक तो यह कि संबंधित उम्मीदवार किस जाति का है (अर्थात् कांग्रेस का ‘क’ उम्मीदवार राजपूत है और भाजपा का ‘ख’उम्मीदवार कुर्मी जाति का है) और चुनाव क्षेत्र की जातिगत संरचना यह है (“अर्थात् एक लाख यादव हैं, 50,000 पासवान हैं, और 40,000 कोरी हैं”).
अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं. विभिन्न समुदायों के बीच पहचानी जा सकने वाली भिन्नताएँ साफ़ तौर पर पहचानी जा सकती हैं या नहीं. जहाँ एक ओर हमने हिंदुओं में कुछ व्यवस्थित भिन्नताएँ पायी हैं, वहीं हमने यह भी पाया है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को सभी तरह के मतदाता आसानी से पहचान लेते हैं. एक स्तर पर इसकी उम्मीद तो की ही जा सकती है. अधिकांश मामलों में तो उनके नामों से ही उनकी पहचान हो जाती है. फिर भी एक पेच है. मुस्लिम उम्मीदवारों की तो आसानी से पहचान हो जाती है, लेकिन मुस्लिम मतादाता भी राजनीतिज्ञों को अच्छी तरह से पहचानते हैं. केवल 13 मुस्लिम मतादाताओं ने ही उम्मीदवारों को पहचानने में गलती की ( जबकि इसकी तुलना में 32 प्रतिशत हिंदुओं ने उम्मीदवारों को पहचानने में गलती की.) इस संख्या की सार्थकता इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि अधिकांश मामलों में मुस्लिम मतादाताओं ने गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दिया. हालाँकि इन परिणामों की अभी अच्छी तरह छानबीन करने की ज़रूरत है. इसका संबंध इस तथ्य से भी है कि मुस्लिम मतादाताओं के वोट अधिकांशतः अनिर्णीत ही बने रहते हैं और यही कारण है कि मुस्लिम मतादाताओं का उम्मीदवारों से संपर्क रहता है.
क्या यह भी मुमकिन है कि ये पैटर्न पैटर्न न होकर सिर्फ़ सुनी-सुनी बातों पर आधारित धारणाएँ हों. लेकिन ऐसा नहीं है. जैसा कि आरंभिक अध्ययन में दर्शाया गया है कि हमने मतदाताओं की गलतियों का साफ़ पैटर्न भी देखा है. शुरुआत में सह-जातीयता के कारण पहचानने में सुविधा रहती है और इसी तथ्य से इस धारणा को भी बल मिलता है कि मतदाता उस समय अधिक सहज रहते हैं जब उन्हें “अपनों में से ही किसी एक को” पहचानना होता है. परंतु 20 प्रतिशत से भी कम मामलों में मतदाता अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देता है. दूसरी ओर शिक्षा के चलते इससे उलट भी होता है. मतदाता जितना अधिक शिक्षित होगा उतनी ही कम संभावना होगी कि वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की जातीय पहचान को पहचान सके. इससे इस धारणा को बल मिलता है कि आधुनिकीकरण और अधिकाधिक आवागमन से संकीर्ण मानसिकता को कम करने में निश्चय ही मदद मिलती है.
उक्त तथ्यों से इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय चुनावों में जातीय पहचान की सशक्त भूमिका अभी भी बनी हुई है. व्यापक स्तर पर किये गये समाज विज्ञान संबंधी शोध-कार्यों से भी इस बात की पुष्टि हुई है. परंतु अब समय आ गया है जब हम सामान्य भारतीयों की जातीय अवधारणा के अपने मॉडल को बदलने पर विचार करें. यदि जातीय संकेत इतना मुखर है तो हमें यह सोचने पर भी बाध्य होना चाहिए कि इसका राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है. क्या मतदाता की गलतियों का राजनीतिज्ञों के अपने मूल्यांकन पर भी असर पड़ता है? क्या इससे मतदाताओं के मन में राजनेताओं से जो उनकी जो अपेक्षाएँ होती हैं, उन पर भी असर पड़ता है, जैसे, उन्हें पद पर रहते हुए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इन प्रश्नों के उत्तर में वे निहितार्थ भी छिपे हैं जिनके कारण हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारतीय मतदाता चाहता क्या है?
मिलन वैष्णव वाशिंगटन डी.सी. में कार्नेई ऐंडोमैंट फ़ॉर इंटरनैशनल पीस के दक्षिण एशिया प्रोग्राम में ऐसोसिएट हैं. आप उनसे Twitter @MilanV पर संपर्क कर सकते हैं.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@hotmail.com>