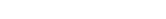हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय ने सन्2012 की जल नीति के राष्ट्रीय प्रारूप से संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के लिए एक स्थायी अधिकरण बनाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया है.जहाँ तक रिपोर्ट का संबंध है, विवादों के निवारण में होने वाले विलंब और बार-बार होने वाले इन विवादों के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय जाने की राज्यों की प्रवृत्ति से सरकार बहुत चिंतित है. न्यायनिर्णयन के लिए स्थायी गुंजाइश रखने का लाभ तो होगा, लेकिन यह काफ़ी नहीं होगा. यह एप्रोच गलत सूचनाओं पर आधारित है. यह एक ऐसा मामला है जिसका नुस्खा तो सही हो सकता है, लेकिन उसका पूर्वानुमान और निदान ठीक नहीं लगता. इसीलिए संदेह होता है कि भविष्य में इससे समस्या का समाधान होगा भी या नहीं. इस संदेह के दो प्रमुख कारण हैं. एक कारण तो यह है कि इसके माध्यम से अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया गया है. यही अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 अधिनियम (IRWDA) के मार्गदर्शी कानून की मूल प्रस्तावना है. स्थायी अधिकरण के कारण समय सीमा की पाबंदियों के बावजूद कानूनी प्रक्रिया और भी बढ़ सकती है. दूसरा कारण यह है कि हमने इस संभावना को पूरी तरह से भुला दिया है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद आम तौर पर व्यापक अंतर्राज्यीय संबंधों के लक्षण होते हैं और संघीय लोकतंत्र के (पुनः) निर्माण में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य के संबंधों के बदलते परिवेश में इनकी भूमिका को अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में स्मरण रखना बेहद ज़रूरी है.
अंतर्राज्यीय जल विवाद के संदर्भ में बदलते अंतर्राज्यीय संबंधों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं: स्वतंत्र भारत में कृष्णा नदी के जल विवाद के निपटारे के लिए तीस वर्ष के अंतराल में दो अधिकरण बने थे, पहला सत्तर के दशक में और दूसरा हाल ही में सन् 2000 के दशक में. सन् 2010 में दूसरे अधिकरण के अधिनिर्णय में अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियाँ उजागर हुईं. अधिकरण ने अपनी पहली कार्यवाही में संबंधित राज्यों के बीच सहयोग-भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, लेकिन अपनी ही कार्यवाही के दौरान भारी असहयोग पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया. अधिकरण ने कहा कि कोई भी राज्य न तो सहयोग करना चाहता है और न ही आपसी सहमति की स्पष्ट संभावना वाले मुद्दों पर भी समझौता-वार्ताओं के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहता है. न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया से जुड़े वकील और टैक्नोक्रेट भी यह मानते हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ इस बात के डर से कि कहीं विरोधी दल उन पर यह आरोप न लगा दे कि उन्होंने राज्य के हितों के साथ समझौता किया है, अंतर्राज्यीय जल संबंधी मामलों पर न तो सहमति प्रकट करने और न ही प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए तैयार होता है. इसके बजाय वे संघर्ष करते हुए, आदेशों की अवहेलना करते हुए और कानूनी प्रक्रिया को अधिक से अधिक खींचते हुए ही राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश में मशगूल रहते हैं. इन प्रवृत्तियों से न केवल न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया का समय खिंचता जाता है, बल्कि अधिकरण के अधिनिर्णयों के अनुपालन में भी बहुत समय लग जाता है. राज्यों द्वारा अधिकरण के न्यायनिर्णय का अनुपालन न करना भी विवाद के निपटारे की एक कमज़ोर कड़ी है और स्थायी अधिकरण होने पर भी यह समस्या बनी रहती है.
अंतर्राज्यीय जल विवाद अब जल आबंटन के प्रतिवाद के लिए नहीं रह गया है, बल्कि अब यह लोकप्रियता हासिल करने और वोट बैंक राजनीति का जबर्दस्त अखाड़ा बन गया है. कावेरी जल विवाद इसका जीता-जागता उदाहरण है कि राजनैतिक दल अब किस तरह अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद का उपयोग करने लगे हैं. अब यह विवाद अदालतों और न्यायाधिकरणों के बंद दरवाज़ों में नहीं होता, बल्कि अक्सर सार्वजनिक मंचों पर ही लड़ा जाता है. तमिल और कन्नड़ लोगों की पहचान और हितों के बीच बढ़ते संघर्ष से उत्पन्न विवादों के कारण नागरिक असंतोष की वारदातें बार-बार होने लगी हैं. दोनों राज्यों के राजनैतिक दल नियमित रूप से अपनी माँगों को प्रचारित करते हैं, अपने पूर्वाग्रहों को लोगों के सामने रखते हैं और उप-राष्ट्रीय राजनैतिक कल्पनाओं के आधार पर लोगों से अपील करते हैं. इसी राजनीति के कारण नये-नये विवाद जन्म लेते हैं और इन्हीं विवादों के कारण राजनीति होती है. इसी राजनीति के कारण राजनैतिक मान्यताएँ बनती हैं और केंद्र और राज्य के दलों से उनके राजनैतिक रिश्ते बनते हैं. इसीके परिणामस्वरूप अंतर्राज्यीय जल विवाद जन्म लेते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है और वे समाप्त भी हो जाते हैं. इसके अलावा, लगातार बढ़ती क्षेत्रीय शक्तियों के कारण उप-क्षेत्रीय हितों का ध्रुवीकरण होता है और राज्यों के बीच बढ़ते प्रतियोगी हितों के मामले ऐसी राजनीति के लिए ईंधन का काम करते हैं. अक्सर ऐसी राजनीति संवैधानिक और प्रशासनिक संकट भी पैदा कर देती है. उदाहरण के लिए कर्नाटक में जारी एक अध्यादेश के अनुसार अधिकरण के सन् 1991 के एक आदेश की अवहेलना कर दी गयी थी या सन् 2004 में हरियाणा के साथ जल साझा करने के करारों को पंजाब के एकपक्षीय निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था.
ऐसी राजनीति कानूनी संदिग्धताओं और अपर्याप्तताओं के बल पर ही फलती-फूलती है. अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के तंत्र के विकास की ऐतिहासिक परिस्थितियों की यही परिणति है. वर्तमान तंत्र का संबंध साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत उठने वाले अंतःप्रादेशिक जल विवादों से जुड़े अपवादवाद से है. सन् 1934 में गठित संवैधानिक सुधार समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि अंतःप्रादेशिक जल विवादों को फ़ैडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया जाना चाहिए. इसका तर्क कोर्ट की कार्यविधि के माध्यम से सुने जाने वाले जल विवादों के असंतोषजनक परिणामों के इतिहास पर आधारित था. लेकिन यह भी हो सकता है कि इम्पीरियल शासन की कदाचित् यही मंशा रही हो कि उनका अधिकार अक्षुण्ण बना रहे. समिति ने सिफ़ारिश की थी कि विवाद के निपटारे का विवेकाधिकार गवर्नर-जनरल का होना चाहिए और यह बात ब्रिटिश इंडिया के प्रदेशों और रियासती राज्यों के बीच के विवादों पर भी लागू होती थी. फ़ैडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अंतर्राज्यीय जल विवाद को अलग रखने का मुद्दा भारत सरकार अधिनियम, 1935 और संविधान के प्रारूप में भी ज्यों का त्यों रखा गया. संविधान सभा ने इन उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभव की और संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत यह ज़िम्मेदारी संसद को देना स्थगित कर दिया. इसके अंतर्गत ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी बाहर रखा गया. बाद में संसद ने इस अनुच्छेद के अनुपालन के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (IRWDA) बना दिया.
अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (IRWDA) के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद (IWD) के अधिनिर्णयन के लिए एक समय के लिए तदर्थ अधिकरण की स्थापना करने की व्यवस्था की गयी. इस अधिनियम में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर भी रोक लगा दी गयी और उच्चतम न्यायालय की डिक्री के ज़रिये ही अधिकरण के निर्णय व्यवस्था कर दी. विधिनिर्माताओं ने निम्नलिखित दो स्पष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर तदर्थ अधिकरण के मार्ग को अपनायाः (क) राज्यों के बीच विरोधी और कानूनी कार्यवाहियों को रोकना, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में बहुत समय लगता है;(ख) विवेकाधिकार और विचार-विमर्श की प्रक्रिया के द्वारा जल्दी और अंतिम निर्णय किया जा सके.
स्थायी अधिकरण की स्थापना से स्थायी तौर पर कानूनी व्यवस्था की गुंजाइश हो सकती है. समय-सीमा के बंधन से बहुत मदद नहीं मिलती. कावेरी अधिकरण के अनुभव पर अगर हम विचार करें तो देखेंगे कि सन् 2007 में अंतिम अधिनिर्णय घोषित करने में इसे पूरे सत्रह साल लगे. अधिनिर्णय घोषित होने के बाद भी यह नहीं माना जा सकता कि विवाद का निपटारा हो गया है. सन् 2012 में यह विवाद फिर से इतना बढ़ गया था कि उच्चतम न्यायालय को दैनिक आधार पर जल आबंटन की निगरानी पड़ी और तब भी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में ही इसको लेकर मनोमालिन्य और असंतोष बना रहा. दोनों ही राज्यों में तब भी कार्यान्वयन के स्वीकार्य तंत्र को लेकर तनातनी बनी रही. कामचलाऊ तंत्र के अभाव में और कानूनी संदिग्धता के कारण कार्यान्वयन पर भी असर पड़ता है. दूसरी ओर, अपने क्षेत्राधिकार पर लगी पाबंदी के कारण उच्चतम न्यायालय भी अधिकरण का अधिनिर्णय दिलवाने के अलावा अधिक कुछ नहीं कर सकता. राज्य भी खास तौर पर उस दौरान जब मानसून अनुकूल नहीं होता, राजनैतिक विवशता के कारण न्यायनिर्णय का अनुपालन करने में विफल रहते हैं.
अंतर्राज्यीय जल विवाद की राजनीति के संदर्भ में स्थायी अधिकरण जैसे कानूनी समाधानों पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता. लंबी कानूनी प्रक्रिया और शत्रुतापूर्ण अंतर्राज्यीय राजनीति के कारण परस्पर विरोधी नतीजे सामने आने के खतरे मँडराते रहते हैं. किसी भी स्थिति में स्थायी अधिकरण बार-बार होने वाले अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए स्थायी समाधान देने का एक परोक्ष मार्ग ही है. ऊपर वर्णित किन्हीं खास ऐतिहासिक परिस्थितियों का बंदी बने रहने के बजाय अब समय आ गया है कि हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर लगी पाबंदी पर पुनर्विचार करें और उच्चतम न्यायालय को अंतर्राज्यीय जल विवादों पर अधिनिर्णय देने दें. फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा. अंतर्राज्यीय जल विवादों का राजनीतीकरण होता रहेगा और यह महत्वपूर्ण है कि राज्यों के बीच शत्रुतापूर्ण राजनीति की प्रवृत्ति को कम किया जाए. जैसा कि चैंटल मुफ़े न कहा है कि जीवंत लोकतंत्र के लिए सही किस्म की परंपराएँ और संस्थाएँ निर्मित करना बेहद ज़रूरी है ताकि शत्रुतापूर्ण राजनीति को उत्पादक लोकतांत्रिक मूल्यों में परिणत किया जा सके. कानूनी न्यायनिर्णयन के लिए सही किस्म की संस्थाओं का हस्तक्षेप आवश्यक है: प्रत्याशित समझौतों और करारों के लिए और उसके बाद उनके अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए. ऐसे संस्थागत हस्तक्षेप सांझी अंतर्राज्यीय नदियों द्वारा उत्पन्न एक दूसरे पर निर्भरता को प्रोत्साहित करने और संघीय अखंडता को मज़बूत करने के अवसर प्रदान करते हैं.
श्रीनिवास चोक्ककुलावाशिंगटन विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में डॉक्टरेट के प्रत्याशी हैं. वे इस समय नयी दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान केंद्र में कार्यरत हैं. उनसे svas@uw.edu पर संपर्क किया जा सकता है.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@hotmail.com>