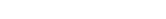यदि आप भारत में समाचारों पर नज़र रख रहे हैं, तो इसकी बहुत कम संभावना है कि मौजूदा विध्वंस पर आपकी नज़र न पड़ी हो. विध्वंस के इस काम में 2022 में उस समय तेज़ी आई थी, जब सरकार ने "न्याय" के बहुसंख्यकवादी स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए विध्वंस का इस्तेमाल किया था. जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश में इसका स्वरूप एक खास तरह का था, वहीं दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर और असम में भी उसी तरह के तरीके आज़माये गए. एक तरफ, "अवैध निर्माण" के आरोपों का इस्तेमाल सीधे तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ किया जा रहा है ताकि उन्हें अधिक से अधिक अलग-थलग किया जा सके. दूसरी ओर, बुनियादी ढाँचे के विकास की अंधाधुंध गति शहर की हरियाली और शहरों में रहने वाली गरीब जनता दोनों के लिए ही खतरा बन गई है.
हम सब जानते हैं कि इस तरह के विध्वंस की शुरुआत नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से नहीं हुई. आधुनिक शहरी नियोजन की कल्पना के बाद से ही योजनाकारों ने अपने स्तर पर नियोजित साफ़-सुथरी छोटी योजनाओं के बाहर या भद्दी दिखने वाली हर चीज़ को विध्वंस के दायरे में लाना शुरू कर दिया था. पेरिस में बैरन हॉसमैन से लेकर दिल्ली में जगमोहन तक सभी ने पूरी निर्ममता से शहर को "योजना" के आकार में लाने का प्रयास किया, भले ही इसके लिए कितने ही लोगों की बलि चढ़ानी पड़े और भारी विनाश का तांडव मचाना पड़े.
ऐसा क्यों है कि आवास का प्रश्न भारत में बमुश्किल ही पैर जमा पाया है? ऐसे विध्वंस का पहला उदाहरण जहाँगीरपुरी में देखने को मिला था, जिसे एक सांप्रदायिक कदम के रूप में देखा गया था और इसे सिविल सोसायटी के भारी गुस्से का शिकार होना पड़ा था. महीने पर महीने बीतते चले गए, लेकिन विध्वंस के काम में कोई कमी नहीं आई. दिल्ली में तुगलकाबाद और असम में सोनितपुर के निवासी विध्वंस का नतीजा आज भी झेल रहे हैं. विस्थापन का दर्द झेलने वाले कामगार अब केवल मुसलमान ही नहीं रह गए हैं. पिछले साल जो लोगों का गुस्सा भड़का था, वह लगता है शांत हो गया है और समाप्त भी हो गया है, लेकिन विध्वंस की वारदातों ने ज़ोर पकड़ लिया है. यहाँ तक कि महामारी के दौरान लागू किये गए लॉकडाउन की शुरुआत में भी जब हमने सैकड़ों हज़ारों प्रवासियों को अपने गाँवों में वापस जाने के लिए पैदल सड़क पर निकलते देखा था. ये दृश्य भयावह होने के साथ ही साथ भ्रमित करने वाले भी थे. जहाँ एक ओर अमेरिकी शहरों में किराया रद्द करने को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर नौकरी जाने के कारण मध्यम वर्ग ने कठिन दौर में भी किराया रद्द करने की आवश्यकता के बारे में मुश्किल से कोई बात कही हो. नीति निर्माताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक और कार्यकर्ताओं से लेकर शिक्षाविदों तक, व्यापक सिविल सोसायटी के लोगों के पास पुनर्वास और कल्याण की माँगों के अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं था.
इसका मतलब किसी भी तरह से यह नहीं था कि आवास से जुड़े कार्यकर्ता इस काम को हीन समझते थे, बल्कि इसका मतलब यह था कि वे यह जानते थे कि उनका काम कितना कठिन है. (1980 के दशक में राष्ट्रीय आवास अधिकार अभियान बैनर के तहत विभिन्न संगठनों के गठबंधन द्वारा एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास के बावजूद) भारत में आवास संबंधी अधिकारों को कभी भी संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया. अदालतें भी आवास संबंधी अधिकारों को मुखर बनाने में अनुकूल नहीं रही हैं. चूँकि हमले अधिक व्यापक और छिन्न-भिन्न हो गए हैं, इसलिए लोगों के लिए संगठित होना कठिन हो गया है और अब सरकार भी सत्ता का एकमात्र केंद्र नहीं रह गई है. आवास संबंधी अधिकार का प्रश्न ऐतिहासिक रूप से भारत में खुद को एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में बदलने में असमर्थ रहा है, जबकि 1968 में पेरिस आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी दार्शनिक हेनरी लेफेब्रे द्वारा दिया गया नारा "शहर की ओर जाने का अधिकार" दुनिया भर के शहरी आंदोलनों में एक लोकप्रिय नारा बन गया है और इसमें स्थानीय संदर्भों के अनुरूप "अधिकार" को परिभाषित करने की छूट भी मौजूद है. इसके फलस्वरूप, "शहर में रहने का अधिकार" पर आधारित ढाँचे का उपयोग किफ़ायती आवास के लिए किया गया है. इन अधिकारों और अन्य अधिकारों की माँग गैर-दस्तावेज़ी श्रमिकों के लिए की गई है. इसे भारतीय संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (UN Habitat) द्वारा पेश किया गया है और आवास को दक्षता और जवाबदेही की भाषा में और सबसे महत्वपूर्ण रूप में एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में व्यक्त करने के लिए इसका विस्तार ऐक्शन एड (Action Aid) और "शहर का अधिकार" (“Right to the City”) द्वारा किया गया है.
इस अंतर का ऐतिहासिक आधार क्या है? जहाँ एक ओर अमरीका में आवास का प्रश्न साठ के दशक से शुरु हुए नागरिक अधिकारों के आंदोलन के केंद्र में रहा, वहीं भारत में देसी राजनैतिक आंदोलनों में आवास के प्रश्न को राजनैतिक मामला नहीं माना गया. जहाँ भारत में आवास का प्रश्न श्रमिकों और जातियों दोनों के ही दिल में रहा है, वहीं श्रमिकों के आंदोलनों और जातिगत आंदोलनों को कामगारों के कार्य “स्थलों” के आसपास ही देखा गया है, लेकिन इसे उनके आंदोलनों के “उद्देश्य” के रूप में सचमुच नहीं देखा गया. 1970 के दशक में कुछ पलों को छोड़कर, जब श्रमिक और दलित दोनों आंदोलनों ने अलग-अलग स्तर पर आवास पर कुछ हद तक ध्यान दिया था, आवास का विषय राजनीति के लिए गौण ही बना हुआ है. इसलिए, भारत में आवास का प्रश्न सामाजिक आंदोलनों की दरारों के बीच ही फँसा रहा है. आवास का सवाल भारत में नब्बे के दशक में ही उठने लगा था. यह वह समय था जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण राजनीतिक परिदृश्य पहले ही बदल चुका था. "सभी के लिए आवास का अधिकार" की स्पष्ट परिभाषा के बिना, आवास का मुद्दा नीतिगत विषय बनकर रह गया और यह एक और सरकारी मामला बनकर रह गया है और इसका आकलन ग्राफ़ के अंतर्गत आँकड़ों में दर्शाया जाने लगा. "शहरों में बसे गरीबों" के स्पष्ट राजनीतिक निर्धारण के अभाव में, बिना किसी पहचान के गरीबी से पीड़ित यह अस्पष्ट आँकड़ा भी भारत में आवास के सवाल को राजनीतिक मुद्दा बनाने में बहुत मददगार नहीं रहा है.
इस नीति-विषयक सरकारी विमर्श का प्रतिवाद वहाँ से हुआ जहाँ इसे बड़े पैमाने पर ऑक्युपेंसी शहरीकरण या ऑटोकंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता रहा है. इससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि गरीब लोगों का शहरी योजनाओं और नीतियों से कोई सरोकार नहीं होता और वे धीरे-धीरे अपना ठिकाना बनाते जाते हैं. भले ही उनके घरों को अवैध करार दिया जाता हो, उनके इस अतिक्रमण को विरोध न मानकर हमारे शहरों की आवास की समस्या का व्यावहारिक समाधान ही मानना चाहिए. जब सरकार के लिए गरीबों को पर्याप्त, सुविधाजनक और किफ़ायती मकान देना संभव न हो तो इन झोपड़पट्टियों को ही अच्छी तरह से नियमित करके उनका सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया जाना चाहिए.
यह न्यायसंगत तर्क कई वर्षों से कई आवास अधिकार संबंधी कार्यकर्ताओं द्वारा पेश किया गया है. हालाँकि यह नीति के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस स्थिति को समस्या के एकमात्र समाधान के रूप में नहीं देखा गया है. आज जिस तरह से हिंसक रूप में उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उसके खिलाफ़ आवास संबंधी अधिकारों के लिए मुखर राजनीतिक भाषा का प्रयोग क्षीण होता जा रहा है. वास्तविकता तो यह है कि इस तरह की कार्रवाई का व्यापक विरोध नहीं हुआ है. केवल कुछ बेअसर अपीलें होती रही हैं और स्पष्ट एवं मुखर राजनीतिक भाषा के अभाव में लोग हिम्मत हारकर समर्पण कर देते हैं. हालाँकि शांत और अहिंसक सत्याग्रह ही इसका अचूक उपाय है, लेकिन जब सरकार इस तरह के संगठित, शांत और अहिंसक सत्याग्रह को दबाने के लिए हिंसक उपाय करने लगे तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं. इसके बिना इस तरह के विध्वंस को रोकने का कोई उपाय नहीं है और लॉकडाउन लगाना तो अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन ही है.
यह देखा गया है कि जब भी सरकार ने पिछले दो दशकों में किसी भी राजनैतिक आंदोलन को रोकने के लिए हिंसक रुख अपनाया है तो उसमें उसे सफलता नहीं मिली है. कई अन्य आंदोलन भी आज चौराहे पर खड़े हैं और उन्हें कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सरकार के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है. ऐसे आंदोलनों में नारीवादी आंदोलन भी शामिल हैं. ऐसे हालात में, हमें न्याय की सार्थक भाषा के इर्द-गिर्द प्रति-विमर्श करने के लिए एक इंटरसैक्शनल भाषा गढ़नी होगी, जिसमें श्रमिक, वर्ग, जाति, लिंग और उससे परे के सभी सरोकारों को एक साथ लाया जा सके. इस संबंध में आवास संबंधी अधिकारों के लिए राजनैतिक दृष्टि से एक ऐसी संतुलित माँग रखनी होगी जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों और संस्थागत हिंसा को रोकने के साथ-साथ श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े सरोकारों की चिंता की जाए और लैंगिक न्याय की व्यवस्था की जाए. इसलिए आवास संबंधी न्याय के लिए आवश्यक है कि भारत के सभी सामाजिक आंदोलनों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहे और एक ऐसी भाषा गढ़ी जाए जिसके माध्यम से आज के इस दौर में कदाचित् एक राजनैतिक भविष्य का उदय हो सके.
सुष्मिता पति बैंगलोर स्थित नैशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया युनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान की सहायक प्रोफ़ेसर हैं.
हिंदी अनुवादः डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (हिंदी), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
Hindi translation: Dr. Vijay K Malhotra, Director (Hindi), Ministry of Railways, Govt. of India
<malhotravk@gmail.com> / Mobile : 91+991002991/WhatsApp:+91 83680 68365