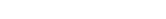भारत-अफ़गानिस्तान के संबंधों की पूरी ताकत का प्रदर्शन 4 दिसंबर, 2016 को अमृतसर में आयोजित छठे हार्ट ऑफ़ एशिया के सम्मेलन में हुआ था. अफ़गान केंद्रित हक्कानी नैटवर्क से संबद्ध “आंतकवादियों” को और भारत केंद्रित लश्कर-ए-ताइबा और जैश-ए-मोहम्मद को “सुरक्षित पनाह” देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए नई दिल्ली और काबुल ने इस मंच का इस्तेमाल इस्लामाबाद को अलग-थलग करने और नीचा दिखाने के लिए सफलतापूर्वक किया. दोनों देशों ने एयर कार्गो के लिए एक ऐसे कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की, जिसमें पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान को उनके देश से भारतीय बाज़ारों में और भारतीय बाज़ारों से उनके देश में आवाजाही का रास्ता अभी तक खुल नहीं पाया है.
जहाँ भारतीय नीति-निर्माता अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ़ गनी के सन् 2014 में पाकिस्तान के प्रति “झुकाव” के कारण चिंतित थे, वहीं 2016 में काबुल के इस बदले हुए बर्ताव से वे खुश भी हो गए हैं. उदाहरण के लिए, जून में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हेरात में भारत-अफ़गानिस्तान दोस्ती बाँध का उद्घाटन किया था. अगस्त में अफ़गानी नेत़ृत्व ने बलोचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में मोदी के बयान का समर्थन किया था. काबुल ने आगे बढ़कर पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार भी किया था और उड़ी में हुए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में सीमापार के साथ-साथ भारत के हैरतअंगेज़ “सर्जिकल हमले” का समर्थन भी किया था.
अफ़गानिस्तान में अपने-अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ये संकेतक भारत-अफ़गानिस्तान की दोस्ती की बढ़िया मिसाल पेश करते हैं. लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे अनेक कारण भी हैं, जिनकी वजह से काबुल की इस “धुरी” के संबंध में सब कुछ ठीक-ठाक है, ऐसा मानकर नहीं चला जा सकता, भले ही इस्लामाबाद के साथ काबुल के संबंधों में कितनी ही गिरावट क्यों न आ गई हो. इसका कारण यह है कि काबुल और नई दिल्ली में पाकिस्तान के संबंध में चलने वाली शांति-वार्ताओं की अंतर्धारा एकतरफ़ा पाकिस्तानी-विरोधी हो सकती है. इन देशों के बीच कभी-कभार चलने वाले संवादों से क्षेत्रीय भू-राजनैतिक गतिशीलता का संकेत मिलता है.
तार्किक दृष्टि से तो यही लगता है कि इस्लामाबाद के साथ अच्छे संबंध होने पर ही भारत और अफ़गानिस्तान दोनों ही देशों में शांति, स्थिरता और विकास हो सकता है. और इतिहास भी यही बताता है कि अफ़गानिस्तान और भारत दोनों ही अवसरों की तलाश में हैं. भले ही दोनों देशों के बीच कितनी ही तल्खियाँ क्यों न रही हों, पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों को उन्हें सुलझाना ही होगा. अफ़गानिस्तान के साथ भारत के स्वातंत्र्योत्तर इतिहास में ऐसे प्रसंगों की भरमार है, जब काबुल और नई दिल्ली पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर चोट पहुँचाने को लेकर एहतियात बरतते रहे हैं. इस बारे में खास तौर पर साठ और सत्तर के दशकों के दो ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों को उद्धृत किया जा सकता है, जिनसे सीख ली जा सकती है.
सबसे पहले पैंसठ के भारत-पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में अफ़गानिस्तान की प्रतिक्रिया नई दिल्ली की दृष्टि से ठंडी और अनिश्चित थी. लाहौर पर लगभग कब्ज़ा कर लेने के बाद भारत राजनयिक दृष्टि से पाकिस्तान को चुनौती देते हुए संयुक्त राष्ट्र में वाद-विवाद के दौरान बलोच, पख्तूनिस्तान और पूर्व पाकिस्तान का सवाल उठा रहा था. युद्ध के दौरान कांग्रेस के कई नेता तो अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि वे नैतिक और राजनयिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर पख्तून और बलोच अलगाववादियों को “ठोस” समर्थन प्रदान करें. काबुल में बाछा खान के साथ उच्च-स्तरीय बैठक करके तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने एक संयुक्त संसदीय बैठक में सीमांत गाँधी को भारत आने का निमंत्रण भी दे डाला था कि वे नई दिल्ली से पख्तूनिस्तान के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएँ और इस बारे में उन्हें सभी दलों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था.
अपनी उदारता के चोले को हटाकर भारत के पख्तूनिस्तान को लेकर अपनाए गए आक्रामक रुख से काबुल में भी काफ़ी हलचल मच गई थी. हालाँकि आम अफ़गानी जनता भारत के पक्ष में थी, लेकिन लाहौर पर हमले के कारण अफ़गानी बादशाह ज़ाहिर खान भयभीत हो गए थे. कसी हुई रस्सी पर चलते हुए उन्होंने अपनी निष्पक्षता बनाये रखने की कोशिश की थी. तथापि भारत की सैन्य सफलता ने अफ़गानों के मन में कम से कम दशहत तो भर ही दी थी और उन्हें पाकिस्तान की हार का भान भी होने लगा था. कालक्रम के अनुसार, जैसे ही भारत ने पख्तूनिस्तान पर अपने राजनयिक हमले शुरू किये और आकाशवाणी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र पख्तूनी विद्रोहियों की गतिविधियों का प्रसारण शुरू किया, काबुल ने भी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में इस मुद्दे पर संयम बरतना शुरू कर दिया था.
अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रालय के राजनैतिक मामलों के महानिदेशक और वरिष्ठतम अधिकारी रवान फ़रहादी ने अमरीका के राजनैतिक राजनयज्ञों को सूचित कर दिया था कि काबुल की तटस्थता के कारण पाकिस्तान में सद्भावना का ऐसा वातावरण बन गया है कि पख्तूनिस्तान के मसले को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है. काबुल की इच्छा थी कि इस्लामाबाद के साथ गतिरोध को खत्म किया जाए और डुरंड रेखा को इस शर्त पर मान्यता देने के लिए लगभग स्वीकार ही कर लिया था कि इस्लामाबाद पख्तूनों को उनके इलाके में रहने के लिए पूरी स्वायत्तता प्रदान करे. भारत के साथ सहयोग करने के बजाय काबुल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस्लामाबाद के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने का इस तरह से प्रयास किया जिससे दोनों देशों को लाभ हो.
यह भू-राजनैतिक जटिलता तब और भी स्पष्ट हो गई जब फ़रहाद ने पाकिस्तान के बिखराव की आशंका से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में व्यंग्य से कहा, “क्या आप समझते हैं कि हम भारत को खैबर दर्रे में आने देना चाहेंगे?” हालाँकि युद्धविराम की घोषणा के तुरंत बाद ही फ़रहादी ने काबुल में व्यक्तिगत तौर पर भारत के राजदूत से कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान का कभी समर्थन नहीं किया और वे दृढ़तापूर्वक भारत के साथ खड़े हैं. कुछ ही दिनों के बाद अफ़गान राजनयज्ञ ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में रहने वाले पख्तूनी और बलोची लोगों के आत्म-निर्णय की माँग का समर्थन किया. युद्ध समाप्त होने पर और पाकिस्तान द्वारा दबाव में अफ़गानिस्तान के प्रस्ताव को मानने से इंकार करने के बाद काबुल फिर से भारत के साथ सहयोग की नीति अपनाने लगा.
दूसरी बात यह भी थी कि 1971 में पाकिस्तान को हराने के बाद भी भारतीय नेतृत्व ने इस्लामाबाद के खिलाफ़ “संयुक्त कार्रवाई” करने के अफ़गानी अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया था. सन् 1973 में पूर्व अफ़गानी प्रधान मंत्री दाउद खान ने एक रक्तहीन क्रांति में ज़ाहिर शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था. खान घोर पाकिस्तान-विरोधी और पख्तूनिस्तान का कट्टर समर्थक था और नवंबर 1974 में तो पाकिस्तान की सीमा पर उसने सैनिक घेराबंदी का आदेश भी दे दिया था. दाउद के गैर-ज़िम्मेदाराना रवैय्ये को देखते हुए काबुल का ऊपर से समर्थन करते हुए भी भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान के विखंडन को लेकर चिंतित होने लगा था और जल्द ही 1971 के युद्ध के बाद बलोच और पख्तून लोगों को शुरू की गई प्रच्छन्न सैनिक सहायता भी उसने बंद कर दी.
मार्च, 1975 में नई दिल्ली के अपने बहु-प्रचारित दौरे में दाउद ने कहा था, “अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में केवल एकमात्र राजनैतिक मतभेद यही है कि पख्तून और बलोची भाइयों को उनका न्यायसंगत अधिकार वापस मिलना चाहिए. हमने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ अपने इस मसले को सुलझाने की ख्वाहिश रखी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई भी सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण हमारी यह ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो सकी है.” निजी बातचीत के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से कहा था कि वे पाकिस्तान को पूर्व की दिशा में सैन्य दृष्टि से उलझाए रखे और हम लोग पश्चिम में उनसे लड़ते रहें ताकि इस समस्या को सुलझाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके. इंदिरा गाँधी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.
भारत का यही अनुमान था कि इस्लामाबाद ने आईएसआई निदेशालय के मार्फ़त पाकिस्तान में काबुल अफ़गान विरोधी इस्लामी शरणगाह बनाकर इसका उत्तर दिया था. जिन सबसे अधिक कुख्यात लोगों को पाकिस्तान से मदद मिली, वे हैं जामियत-ए-इस्लामी के अहमद शाह मसूद और बरहनुद्दीन रब्बानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार, जिसने अपना सफ़र तो जामियत से शुरू किया, लेकिन बाद में जामियत-ए-इस्लामी में शामिल हो गया. दिलचस्प बात तो यह है कि जिन लोगों और संस्थाओं को उन्होंने खड़ा किया, वे आज भी अफ़गानिस्तान के राजनैतिक परिदृश्य में वहाँ सक्रिय हैं.
आगामी दशकों में भारत और अफ़गानिस्तान दोनों ने ही पाकिस्तान के साथ वार्ताएँ भी शुरू कीं और लड़ाई भी लड़ते रहे. हालाँकि यह तर्क दिया जा सकता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने के कारण ही भारत की ओर से उस पर हमले का मौजूदा खतरा टल गया, लेकिन उक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो भारत ने और न ही अफ़गानिस्तान ने उप-महाद्वीप में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने से पहले भी अपने क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए सैन्यबल का उपयोग करने पर गंभीरता से कभी विचार किया. जो भी हो, काबुल और काबुल के रणनीतिक मूल्य पर भारत का प्रभाव डालने की नई दिल्ली की अपनी सीमाएँ रही हैं. मौजूदा दोस्ताने का मतलब यही है कि ऐसे हालात में जब भारत पाकिस्तान अपने दोनों पड़ोसी देशों से अलग-थलग पड़ गया है, भारत और अफ़गानिस्तान के हित एक दूसरे से मेल खाने लगे हैं.
सन् 2014 में गनी के पाकिस्तान के प्रति झुकाव के कारण भारतीय नीति-निर्माता ठीक उसी तरह चिंतित हो गए थे, जैसे कि बीसवीं सदी के आरंभ में करज़ई के कार्यकाल में हुआ था. इसका कारण यह नहीं था कि ये दोनों राजनेता अनुभवहीन थे और पाकिस्तान के इरादों से अनभिज्ञ थे, बल्कि उनके इन प्रयासों का कारण था, भूराजनैतिक तनाव, जो इतिहास के पन्नों से आसानी से मिटाया जा सकता है. उक्त प्रकरणों से यह भी उजागर होता है कि भारत डूरंड रेखा पर रणनीतिक संतुलन बनाये रखना चाहता है, लेकिन इस सिद्धांत की कम ही सराहना की जाती है, जबकि कई दशकों से नई दिल्ली की अफ़गानिस्तान के प्रति यही नीति रही है. भारत की क्षमताओं की सीमा को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो भी इस बात में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कई अफ़गानी लोग बहुत लंबे समय से नई दिल्ली की इसीलिए आलोचना करते रहे हैं कि उसने काबुल के समर्थन के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की.
शीत युद्ध की संगठनात्मक परिधि से बाहर निकल कर और तथाकथित आतंक के खिलाफ़ “अमरीका बनाम उन्हें” जैसे विषय पर संवाद करने के लिए भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर जटिल भूराजनैतिक क्षेत्र में पहल शुरू कर दी है. नीति की दृष्टि से इस संवाद में इन देशों की दो मंशाएँ दिखाई देती हैं. रणनीतिक कायाकल्प के जोखिम से बचते हुए अपने लाभ की स्थिति को ज्यों की त्यों बनाये रखना. इससे क्षेत्रीय पुनर्संशोधनवाद का खतरा कम हो जाएगा और रणनीतिक लक्ष्य के बजाय यह राजनयिक हथियार बन जाएगा.
इस्लामाबाद, अपने पड़ोसियों (इसमें चीन भी शामिल है, क्योंकि चीन पर वह इतनी बुरी तरह निर्भर हो गया है कि यह उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है) के साथ संबंधों के निर्वाह में कल्पनाशीलता की कमी के कारण और आतंकवादी समूहों में अंतर करने के कारण भारत-अफ़गानिस्तान “धुरी” को निरंतर मज़बूती प्रदान कर रहा है, जबकि नब्बे के दशक में पाकिस्तान ने इस परिदृश्य को रोकने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की थी. कुछ हद तक यह उसकी राजनैतिक मज़बूरी है और कुछ हद तक उसकी क्षमता की कमी भी है. यही कारण है कि क्षेत्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की माँग के बावजूद और इसके लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में बल प्रयोग करने के बावजूद भी और दक्षिण एशिया के स्थायी भूराजनैतिक अंतर्विरोधों, जो 1998 के बाद बद से बदतर ही होते गए हैं, के बावजूद भी आवश्यकता इस बात की है कि ये देश आपस में मिल-बैठकर अपने गहरे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें. किसी भी भावी युद्ध ( जिसकी फ़िलहाल आशंका नहीं है) के लिए बार-बार बदलते हुए रिश्ते खतरनाक साबित हो सकते हैं. इसलिए आवश्यकता इस बात की है इस क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए रणनीतिक रूप में निर्णायक स्थिति बहाल करने की कोशिश की जाए.
अविनाश पालिवाल किंग्स कॉलेज में रक्षा अध्ययन के लैक्चरर हैं और “शत्रु के शत्रुःअफ़गानिस्तान में सोवियत हमले से लेकर अमरीका की सैन्य वापसी तक भारत” के लेखक (लंदनः हर्स्ट पब्लिशर्स, 2017) हैं.
हिंदी अनुवादः डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@gmail.com> / मोबाइल : 91+9910029919