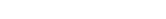कुछ आप्रवासी लेखकों के अनुमान के अनुसार भारत में मौसमी आप्रवासी मज़दूरों की संख्या 100 मिलियन तक भी हो सकती है. आप्रवासी मज़दूरों को न तो सामाजिक सेवाएँ मिलती हैं और न ही ये लोग शहरी इलाकों में स्थायी तौर पर बस सकते हैं. ऐसे हालात में ये आप्रवासी मज़दूर खास तौर पर खेती-बाड़ी के मौसम में गाँवों में ही रहना पसंद करते हैं. इसके फलस्वरूप वे अपनी मज़दूरी के लिए अपने गाँवों और मज़दूरी के ठिकानों के बीच ही भटकते रहते हैं और पूरे साल के दौरान अधिक से अधिक समय घर के बाहर ही गुज़ारते हैं.
एक ओर तो आप्रवासियों के लिए मज़दूरी का काम उनके परिवार के लिए नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलता है, वहीं भारी जोखिम भी पैदा कर देता है. इस जोखिम का सबसे अधिक असर आप्रवासी मज़दूरों के बच्चों को ही झेलना पड़ता है. ये बच्चे अक्सर अपने माँ-बाप के साथ उनके मज़दूरी के काम के ठिकानों पर जाने के लिए विवश होते हैं. कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि भारत में अपने परिवारों पर आश्रित लगभग छह मिलियन आप्रवासी मज़दूरों के बच्चे हर साल अपने माँ-बाप के साथ भटकते रहते हैं. कई मिलियन बच्चों पर इसका परोक्ष रूप में असर पड़ता है और इनमें से अधिकांश बच्चे माँ-बाप की अनुपस्थिति में कोई न कोई घरेलू ज़िम्मेदारी उठाने के लिए विवश होते हैं. दुर्भाग्यवश केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर भारतीय प्रशासन ने आप्रवासी मज़दूरों के बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता नहीं दी है और ये बच्चे उपेक्षित होते रहे हैं और इन बच्चों की अनूठी समस्या को हल करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है.
सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये गये आप्रवासी छात्रावास कार्यक्रम को ही लेते हैं. बुनियादी शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का भारत का यह एक फ़्लैगशिप प्रोग्राम है. इसकी मूल धारणा बहुत सरल हैः स्थानीय विद्यालय के अनुरोध पर उन छात्रों को जो अपने माँ-बाप के साथ आप्रवासन पर भटकने के लिए विवश हो सकते हैं, छह महीने की आप्रवासन-अवधि के लिए प्राथमिक विद्यालय के भवन में रहने की अनुमति दी जा सकती है. सर्व शिक्षा अभियान उसी समुदाय से दो अधिष्ठाताओं (वार्डनों) के वेतन, भोजन और कुछ बुनियादी सप्लाई की सुविधाएँ प्रदान करता है. यह कार्यक्रम बहुत किफ़ायती होता है, क्योंकि इससे उन्हें वे तमाम सुविधाएँ अनायास ही मिल जाती हैं जो स्थानीय विद्यालय में पहले से ही उपलब्ध होती हैं. इस कार्यक्रम के प्रतिभागी ऐसे रचनात्मक परिवेश से लाभान्वित हो सकते हैं और वहाँ पर वे अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा सकते हैं और अपने गाँव की सुरक्षा के घेरे में भी रह सकते हैं.
दुर्भाग्यवश प्राथमिकताओं में बदलाव होने के कारण केंद्र सरकार ने राजस्थान के अस्सी आप्रवासी छात्रावासों को आगामी वर्ष से निधि का वित्तपोषण करने से इंकार कर दिया है. यों तो सर्व शिक्षा अभियान के बजट का यह बहुत ही मामूली-सा ही हिस्सा है, लेकिन इससे राजस्थान के कई गरीब परिवारों के बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा.
दक्षिणी राजस्थान में मेरे फ़ील्ड वर्क के साक्ष्य से और आप्रवासी मज़दूरों के लिए बनाई गई सामाजिक संरक्षण की रणनीतियों की समीक्षा से यह पता चलता है कि जिन इलाकों में आप्रवासी मज़दूरों का जन्म होता है वहीं पर आप्रवासी छात्रावासों आदि स्रोत-आधारित हस्तक्षेप से बाल आप्रवासन और बाल मज़दूरी को रोका जा सकता है.
राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के उत्तर और पूर्व में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के गरीब आप्रवासी मज़दूरों के लिए मध्य गुजरात के शहरी इलाके लोकप्रिय ठिकाने रहे हैं. गुजरात के ईंट के भट्टों, निर्माण, सूत की कताई और कृषि उद्योगों के लिए अधिकांश मौसमी मज़दूर इन्हीं इलाकों से आते हैं. दक्षिणी गुजरात में अनुसूचित जनजाति के अनेक परिवार (अधिकांशतः भील और गरसिया जनजाति के ) दो-जून रोटी के लिए आप्रवासन पर ही निर्भर रहते हैं.
भारी गरीबी के कारण आप्रवासी मज़दूरों में महिला आप्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है. डेविड मोस्से के नेतृत्व में सन् 1997 में इस इलाके के आप्रवासन पर किये गये अध्ययन के अनुसार आप्रवासी मज़दूरों में महिलाओं का प्रतिशत 42 है. दक्षिणी राजस्थान में गाँवों में किये गये मेरे सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि गुजरात में आप्रवासन के लिए आने वाले 75 प्रतिशत महिला आप्रवासी मज़दूर और 82 प्रतिशत पुरुष आप्रवासी मज़दूर अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार तो गुजरात में अवश्य आए हैं. जहाँ एक ओर इस इलाके के अनुसूचित जनजाति के लगभग सभी परिवारों के पास कुछ न कुछ ज़मीनें हैं, वहीं उनकी जोत छोटी हैं और अनुत्पादक भी हैं और सिंचाई की सुविधा तो और भी कम लोगों के पास है. एक समय था, जब ये लोग जंगल पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते थे, लेकिन इस इलाके के वन्यीकरण के भारी विनाश के कारण इन समुदायों के पास अब आजीविका के और भी कम अवसर बचे हैं.
इनमें से कुछ लोग तो आप्रवासी मज़दूरी से अपना भरण-पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग स्थानीय साहूकारों के कर्ज़ और आर्थिक असुरक्षा के कारण आर्थिक बोझ से दबे रहते हैं. चूँकि इनकी अधिकतर आमदनी का स्रोत आप्रवासी मज़दूरी ही है, इसलिए दक्षिणी राजस्थान में मनरेगा के कार्यक्रम का इनके परिवारों के आप्रवासी पैटर्न पर बहुत कम असर हुआ है. सर्वेक्षण के अनुसार 79 प्रतिशत प्रौढ़ मज़दूरों ने इस कार्यक्रम में कम से कम एक बार भाग तो लिया ही है, लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर आप्रवासन करके मज़दूरी भी की है.
आजीविका के लिए आप्रवासी मज़दूरी पर निर्भर रहने से परिवार पर भारी बोझ भी पड़ता है. आप्रवासन करने वाले अधिकांश सीमांत समुदायों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सारा परिवार ही कार्यस्थल पर उनके साथ रहे, क्योंकि अपने ही गाँव में बच्चों को छोड़ने के लिए उनके पास कोई ठौर-ठिकाना नहीं रहता. श्रमिक अनुसंधान व कार्य के प्रयास केंद्र के एक अनुमान के अनुसार केवल ईंट के भट्टों पर ही स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 840,000 है. बाँसवाड़ा में मैंने पाया कि 34 आप्रवासी मज़दूर परिवारों के पास कम से कम एक साल में एक बच्चा तो उनके साथ अवश्य ही रहता है. बारह साल की उम्र के बाद बच्चे भी निर्माण स्थलों पर अपने माँ-बाप की मदद करने लगते हैं, लेकिन ईंट के भट्टों पर तो ये बच्चे पाँच साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं. पीसमील मज़दूरी प्रणाली में तो बाल श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलता है.
कार्यस्थलों पर बच्चों को चोट लगने और बीमार पड़ने की आशंका के साथ-साथ वे शोषण के भी शिकार हो सकते हैं.साथ ही वे शैक्षणिक अवसरों से भी वंचित हो जाते हैं. अगर वे शिक्षित हो जाते तो गरीबी के दुश्चक्र से भी छुटकारा पाने की गुंजाइश हो सकती थी. अमेरिकन इंडिया फ़ाउंडेशन (AIF) के वित्तपोषण से चलने वाले अनेक गैर-सरकारी संगठन (NGOs) कार्यस्थलों पर ही बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. कार्यस्थलों के परिवेश को शिक्षा के अनुकूल बनाना आसान नहीं है और इस प्रकार के प्रयासों से बहुत मामूली लाभ ही हो पाता है. तदनुसार तीन राज्यों के बहुत अधिक आप्रवासन वाले इलाकों में आप्रवासी छात्रावास कार्यक्रम चलाने वाले एआईएफ़ ने अपने शिक्षण व आप्रवासन संबंधी कार्यक्रम (LAMP) को स्रोत व गंतव्य दोनों ही क्षेत्रों पर दोहरा ध्यान देने के बजाय पूरी तरह से स्रोत-गाँव केंद्रिक प्रयास शुरू कर दिए हैं.
जिन बच्चों के माँ और बाप दोनों ही आप्रवासी मज़दूरी के लिए गाँव से बाहर चले जाते हैं, उनके कंधों पर अधिकांश या फिर सारी की सारी घरेलू ज़िम्मेदारी आ जाती है. इसके कारण दक्षिणी राजस्थान में ऐसे घरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिनका संचालन बच्चे ही करते हैं. हाल ही में ‘सेव द चिल्ड्रन’ (‘बच्चों को बचाओ’) ने इस पर एक दस्तावेज़ तैयार किया है. माँ-बाप की अनुपस्थिति में बारह साल की उम्र के जो बच्चे घर की पूरी ज़िम्मेदारी सँभालते हैं और छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते हैं, उनके पास स्कूल जाने का समय ही नहीं बचता. बाँसवाड़ा के अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में खास तौर पर दिवाली के बाद आप्रवासन के मौसम के बाद जैसे-जैसे शैक्षणिक सत्र आगे बढ़ता है, छात्रों की उपस्थिति कम होती जाती है. जिन स्कूलों में मैं गई, उनमें से अधिकांश स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट लगभग 25 प्रतिशत था.
राजस्थान में स्कूल न जाने वाले 410,957 बच्चे आप्रवासन के दबाव के कारण स्कूल प्रणाली से ही अलग हो गए. एसएसए द्वारा चलाये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों (STPs) के माध्यम से इन बच्चों को फिर से स्कूल प्रणाली के अंतर्गत लाया जा रहा है. इनके लिए ऐसे सेतु पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें इन बच्चों को शैक्षणिक दृष्टि से स्कूल में उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जाती है. यह काम ठेके पर रखे गए शिक्षकों के लिए जितना कठिन है, उतना ही कठिन उन छात्रों के लिए भी है, जो कुछ साल तक कार्यस्थल पर रह चुके हों. इसलिए इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकांश एसटीपी फ़ेल हो जाते हैं. साल भर तक मैंने बाँसवाड़ा में फ़ील्डवर्क किया. एसएसए को इस ज़िले में एक तिहाई एसटीपी बंद कर देने पड़े. अधिकांश एसटीपी वहीं सफल हुए जहाँ पर आप्रवासी छात्रालय जैसी आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध थीं.
छात्रों को स्कूल प्रणाली के अंतर्गत दुबारा लाना सचमुच एक चुनौती है. खास तौर पर अनुसूचित जनजाति वाले इलाकों में स्कूल न जाने वाले छात्रों की संख्या वहाँ अधिक है, जहाँ आप्रवासन के कारण ड्रॉप आउट होता है. इसलिए ड्रॉप आउट को रोकने के लिए किये जाने वाले प्रयासों पर निवेश करने में ही समझदारी है. आप्रवासी छात्रावास और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय ( जो आवासीय प्राथमिक बालिका विद्यालयों का एक कार्यक्रम है) दो ऐसी संस्थाएँ हैं जो आप्रवासन के कारण होने वाले ड्रॉप आउट को कम करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं. इन दोनों कार्यक्रमों को मान्यता देकर बाल मज़दूरी और ड्रॉप आउट को रोकने की सरकारी रणनीति को सफल बनाया जा सकता है.
रिसर्च एक्रॉस इंडिया आप्रवासी मज़दूर-वर्ग की लगातार बढ़ती तादाद की तस्वीर के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने में जुटा है. इस वर्ग के लोग, खास तौर पर उनके बच्चे जिस तरह का जोखिम झेलते हैं उसके निवारण के लिए आवश्यक है कि भारत इनके विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे मुख्य प्राथमिकता के रूप में घोषित करे. स्रोत-आधारित हस्तक्षेप से ही इन बच्चों को आप्रवासन के भारी जोखिम से बचाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी परिवार आप्रवासन के दबाव के कारण अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए विवश न हो.
मैगन रीड ‘कैसी ’ की अनुसंधान समन्वयक हैं. वह 2012-13 की फ़ुलराइट- नेहरू छात्र रिसर्च फ़ैलो है.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार < malhotravk@gmail.com > मोबाइलः 91+9910029919