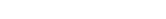सन् 1985 में भारत में गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने प्रसिद्ध उद्गार प्रकट करते हुए कहा था: “सरकार द्वारा आम आदमी के कल्याण पर खर्च किये गये एक रुपये में से सिर्फ़ सत्रह पैसे ही आम आदमी तक पहुँचते हैं.” इस तरह के मूल्यांकन से प्रेरित होकर सन् 1993 में 73 वाँ संशोधन पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर सीमित रूप में ही सही, चुनावों को अनिवार्य बनाया गया और ग्राम पंचायतों में सरपंचों का चुनाव सीधे स्थानीय लोगों द्वारा किया जाने लगा. भारत सरकार के इस प्रयास के कारण शासन को आम आदमी के पास लाने का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और इस बात की उम्मीद बँधने लगी कि सरकार की नीतियों का लाभ सीधे आम जनता को मिलने लगेगा. दो दशक के बाद क्या हम दावे के साथ कह सकेंगे कि विकेंद्रीकरण के कारण गरीब-समर्थक नीतियों को प्रोत्साहन मिलने लगा है?
हाल ही के वर्षों में कुछ सुधार होने के बावजूद शोधकार्यों से पता चलता है कि गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के रूप में प्रचारित नीतियों से गरीबों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है. उदाहरण के लिए, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों को आबंटित होने वाले बीपीएल कार्डों के आबंटन पर विचार करें. यह एक ऐसी पात्रता है, जिसके अनुसार अनाज से लेकर स्वास्थ्य-सेवा तक व्यापक पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है. 2009 के EPW लेख में बताया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 5 बीपीएल कार्डधारकों में से 2 कार्डधारकों की सब्सिडी अधिकाशतः ऐसे लोगों के हाथों में पहुँच गई है, जो गरीब नहीं हैं, जबकि यह सब्सिडी केवल गरीबों के लिए ही थी और इस प्रकार अधिकांश गरीबों को यह कार्ड ही नहीं मिल पाया. हालाँकि इन निष्कर्षों के आधार पर गरीबों की सही पहचान न कर पाने के कारण हम स्थानीय राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों या सिस्टम को भी दोषी सिद्ध नहीं कर सकते. आम धारणा यही है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख या सरपंच ही अपने विवेकाधिकार से बीपीएल कार्ड का वितरण करते हैं और इससे वे स्वयं ही समृद्ध होते हैं या वे अपने समर्थकों को पुरस्कृत करते हैं या अपनी बिरादरी या परिवार-जनों को लाभ पहुँचाते हैं. इससे शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं को इस बात का साक्ष्य मिला कि भारत में स्थानीय राजनीतिज्ञों या ग्रामीण आर्थव्यवस्था के प्रभावशाली लोगों ने गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को हथिया रखा है और गरीबों के कल्याण की बात उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है.
स्थानीय राजनीतिज्ञों की इस निराशाजनक तस्वीर का प्रभाव अंततः नीति-निर्माण पर पड़ता है और समस्या के सही निदान न हो पाने की भी यही वजह है. पहली बात तो यह है कि भारत जैसे विकासशील देशों की केंद्रीय सरकारों के पास न तो इतने संसाधन हैं कि वे सभी गरीब परिवारों को लाभान्वित कर सकें और न ही इतनी क्षमता है कि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों का लाभ केवल गरीबों तक ही पहुँचे.
इससे यह स्पष्ट है कि स्थानीय नौकरशाहों या राजनीतिज्ञों के विवेकाधिकार को बदला नहीं जा सकता. दूसरी बात यह है कि हम बीपीएल कार्डधारकों के आबंटन जैसे नीतिगत परिणामों पर स्थानीय राजनीतिज्ञों की प्राथमिकताओं को न तो बदल सकते हैं और न ही ऐसी कोई रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञों और विभिन्न सरकारी पदों पर आसीन नौकरशाहों के साथ-साथ सरपंच के पास भी आबंटन की सीमित शक्तियाँ हैं. इसके फलस्वरूप बेहतर यही होगा कि नीति-निर्माता स्थानीय नेताओं पर ही इसका निर्णय छोड़ दें. क्योंकि पहले स्तर पर ही स्थानीय नेताओं की प्राथमिकताएँ गरीब-समर्थक होती हैं.
भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अपेक्षाकृत आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप नीलांजन सरकार और मैंने अगस्त, 2015 को ‘कैसी’के वर्किंग पेपर में दर्शाया था कि ग्रामीण परिवेश के मतदाता स्थानीय निष्पक्ष चुनावों में खुलकर और बिना किसी दबाव के उन्हीं राजनीतिज्ञों को ही चुनते हैं जिनकी प्राथमिकता में गरीबों के कल्याण की भावना निहित रहती है. इसके अलावा, हमने यह तर्क भी सामने रखा है कि विविध जातियों वाले ग्रामीण भारत में मतदाता अपनी ही जाति या बिरादरी के चिर-परिचित उम्मीदवारों के बजाय उदार विचारों वाले उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं.
यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हम वितरक प्राथमिकताएँ मतदाताओं के उन वर्गों को मानते हैं जिन्हें सरपंच नकदी या मकान आदि की सीमित सुविधाएँ देना पसंद करते हैं.नीतिगत परिणामों के निष्कर्षों के ठीक विपरीत, हम मूलतः प्राथमिकता-प्राप्त उन नेताओं को लेकर चिंतित हैं जो संभावित लाभार्थी हो सकते हैं. इसका आकलन करने के लिए हमने 2013 के कम आमदनी वाले चौरासी ग्राम पंचायतों के अपने सर्वेक्षण में एक प्रयोगशाला-खेल को भी शामिल किया है. इस खेल में, सरपंचों से कहा जाता है कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी रकम को पाँच टोकन में बाँट लें, जिनसे 200 रुपये का कोई पुरस्कार विजेता प्रभावित होता हो. चूँकि हर मतदाता को कम से कम एक लॉटरी अवश्य मिलती है और लॉटरी के इनाम के वितरण को गुप्त रखा जाता है, इसलिए हमारे उपाय पर सामाजिक दबाव या चुनावी रणनीति का कोई असर नहीं होता.
अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार गरीब ग्रामीण लोग स्थानीय चुनावों में गरीब-समर्थक स्थानीय नेताओं का ही चुनाव करने में सफल होते हैं. पहली बात तो यह है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के विपरीत इस चुनाव में सबको सब कुछ पता होता है. मतदाता और सरपंच पद के लिए खड़े उम्मीदवार मतदान केंद्रों पर जाते समय आपस में एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं. हमारे आँकड़ों के अनुसार लगभग 95 प्रतिशत मामलों में सरपंच मोटे तौर पर अपनी ग्राम पंचायतों के सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानते ही हैं. दूसरी बात यह है कि चूँकि सरपंच या उनके परिवार के निकट संबंधी अक्सर पिछले चुनावों में भी निचले स्तर पर बिचैलियों का काम करते रहे हैं, इसलिए मतदान केंद्र में जाने से पहले ही मतदाता अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कौन गरीब-विरोधी है और कौन गरीब-समर्थक. तीसरी बात यह है कि भारत के ग्रामीण जीवन की यही विशेषता है कि ग्रामीणों का सामाजिक तानाबाना बहुत गहरा होता है. गरीब और न्यूनतम आजीविका पर आधारित जिन गाँवों का हमने अध्ययन किया है, हमने पाया है कि औसत मतदाता बहुत गरीब होने के साथ-साथ सबसे गरीब ग्रामीणों से भी सामाजिक तौर पर जुड़ा होता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि औसत मतदाता की प्राथमिकता गरीबोन्मुखी है. राजनीति विज्ञान संबंधी शोध के प्रमुख निष्कर्ष यही हैं कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को जीतने के लिए औसत मतदाता से ही जुड़ना होगा. इसी तर्क से मतदाता भी ऐसी प्राथमिकता वाले राजनीतिज्ञों का पता लगा सकते हैं जो किसी खास जाति या परिवार-समूह से जुड़े होते हैं. ग्रामीण भारत जैसे विविध जातियों के मिले-जुले चुनाव-क्षेत्रों में जीतने के लिए व्यापक (बहु-जातीय) वितरक प्राथमिकताएँ ही आवश्यक हैं. हमारे आँकड़े इन अपेक्षाओं का दृढ़ता से समर्थन करते हैं.
जहाँ एक ओर इन परिणामों से आशावाद का संकेत मिलता है, वहीं स्थानीय चुनावों से अपने समर्थकों के साथ पक्षपात करने वाले सरपंच को भी नहीं खोजा जा सकता. हमारे निष्कर्ष के अनुसार जिन्हें समर्थक माना जाता है, उऩकी तादाद संभावित गैर-समर्थकों की तुलना में 3.6 गुना अधिक होती है. जब हम सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर गौर करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरपंच गरीब गैर-समर्थकों की तुलना में दुगुने गरीब समर्थकों तक पहुँच बनाते हैं. वस्तुतः वे गरीब गैर-समर्थकों की तुलना में संपन्न समर्थकों तक थोड़ी अधिक पहुँच बनाते हैं.
गरीब ग्रामीण परिवेश में स्थानीय लोकतंत्र बहुत दृढ़ता के साथ गरीब-समर्थक प्राथमिकताओं को प्रोत्साहित कर सकता है और इसीसे यह संभव हो पाएगा कि मतदाता गरीब-समर्थक उम्मीदवारों का ही चुनाव करें. इससे यह स्पष्ट है कि निर्वाचित राजनीतिज्ञों की आबंटन की शक्ति को बढ़ाने से अनिर्वाचित स्थानीय एजेंटों (अर्थात् नौकरशाहों) की शक्ति बढ़ती है, जबकि स्थानीय निर्वाचित निकायों की शक्ति बढ़ाने से संपन्न लोगों को लाभान्वित करने के बाहरी दबाव को झेलने की उनकी शक्ति बढ़ जाती है. विवेकाधिकार और राज्य की कमज़ोर ताकत के संदर्भ में हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि गरीब गैर समर्थकों को कैसे अलग किया जाए. विवेकाधिकार को सीमित करके या गरीब-समर्थक उपायों को बढ़ाकर ही इस समस्या का निदान खोजा जा सकता है.
मार्क शेंदर स्वार्थमोर कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विज़िटिंग प्रोफ़ेसर हैं और ‘कैसी’के नॉन-विज़िटिंग स्कॉलर हैं. उऩका संपर्कसूत्र है mschnei1@swarthmore.edu.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@gmail.com> / मोबाइल : 91+9910029919