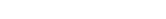जैसे-जैसे काबुल रावलपिंडी के साथ मेल-मिलाप की कोशिश कर रहा है, भारत की अफ़गानिस्तान-नीति में बदलाव दिखाई देने लगा है. अफ़गानी अधिकारियों के कई बार निवेदन करने पर भी दिल्ली अक्तूबर, 2011 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित और बहुचर्चित द्विपक्षीय रणनीतिक करार पर चर्चा करने और उसकी समीक्षा करने के लिए द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी परिषद की बैठक आयोजित करने से हिचक रहा है. 2-3 सितंबर 2015 को काबुल में आयोजित छठे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा भाग न लेने के कारण इस ज़ख्म पर मानो नमक छिड़क दिया गया है. कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशऱफ़ घानी के पाकिस्तान के प्रति बढ़ते रणनीतिक झुकाव के कारण भारत के अधिकारी बहुत रुष्ट हो गए हैं. अगर यह सच है तो भी यह पहला अवसर नहीं है जब भारत की अफ़गानिस्तान के प्रति बेरुखी बढ़ रही है. 1990 के दशक में और 2000 के आरंभिक दशक में भी जब अफ़गानिस्तान का गृहयुद्ध अपने चरम पर था तब भी इस तरह की बेरुखी बार-बार दिखाई पड़ती थी.
अफ़गानिस्तान संबंधी भारत की नीति के तीन मुख्य बिंदु हैं, जो अक्सर आपस में गुँथे रहते हैं. पहला बिंदु है दिल्ली की यह इच्छा कि वह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाकर रखे. अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता और निकटता, जैसी कि नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में तालिबानी शासन के दौरान दिखाई देती थी, भारत के रणनीतिक हित में नहीं है.
दूसरा बिंदु है अफ़गानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ना. काबुल के प्रति सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करते हुए काबुल के प्रति भारत की नीति अक्सर बाहरी दबावों के कारण भी आकार ग्रहण करती रही है. उदाहरण के लिए सन् 2001 में बोन सम्मेलन में अमरीकी नेतृत्व में नैटो सैनिक हस्तक्षेप के बाद हामिद करज़ई के नेतृत्व को स्वीकार करके भारत ने एक प्रकार से समझौता ही किया था. भारतीय अधिकारी सत्ता के शिखर पर एक ऐसा प्रत्याशी देखना चाहते थे जो तालिबानी संयुक्त मोर्चे का विरोधी हो, लेकिन अंततः उसे अमरीकी दबाव में करज़ई के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ा.
अफ़गानिस्तान के प्रति भारत की नीति को संचालित करने वाला तीसरा बिंदु है, अफ़गानिस्तान में होने वाली राजनैतिक उथल-पुथल, जिसके कारण अफ़गानिस्तान के विभिन्न राजनैतिक गुट भारत के साथ संपर्क बनाने को इच्छुक रहते हैं. अफ़गानी लोगों में भारत के प्रति जबर्दस्त सद्भावना होने के बावजूद अफ़गानिस्तान के विभिन्न राजनैतिक गुट भारत के प्रति अलग-अलग रुख अपनाते रहे हैं. जहाँ एक ओर करज़ई दिल्ली की मेज़बानी गर्मजोशी से करते रहे हैं, वहीं घानी प्रशासन भारत के प्रति बेरुखी दिखाता रहा है.
अफ़गानिस्तान के संदर्भ में जब भी भारत की आंतरिक नीति को लेकर कोई बहस छिड़ती है तो इन्हीं तीनों बिंदुओं के मिले-जुले स्वरूप के इर्द-गिर्द ही बहस सिमटी रहती है. भारत के कुछ अधिकारी,जिन्हें हम “कट्टरपंथी” कह सकते हैं, पाकिस्तान-विरोधी सभी गुटों को राजनैतिक और वित्तीय समर्थन देने के पक्षधर हैं. यह बिंदु भी विचारणीय है कि करज़ई या 9/11 से पहले संयुक्त मोर्चे के साथ भारत के संबंध बेहद सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं और अस्सी के दशक में पूर्व साम्यवादी सरकारें भी पाकिस्तान विरोधी रही हैं. कट्टरपंथी यह मानते हैं कि पाकिस्तान समर्थक अफ़गानी गुटों से बात करना फिज़ूल है, क्योंकि इन गुटों पर रावलपिंडी की पकड़ बहुत मज़बूत है.
दूसरे अधिकारियों को हम “समझौतावादी ” कह सकते हैं, जो यह मानते हैं कि अफ़गानी सरकार का पाकिस्तान के प्रति कैसा भी रुख क्यों न हो, हमें सभी अफ़गानी गुटों से बातचीत करते रहना चाहिए. समझौतावादी यह मानते हैं कि ऐसी नीति अपनाकर ही अफ़गानिस्तान की घरेलू राजनीति में स्थायित्व लाया जा सकता है और काबुल और इस्लामाबाद के प्रति कुछ हद तक रणनीतिक समानता लाई जा सकती है. यह नीति अपनाकर भारत यह सुनिश्चित कर सकेगा कि काबुल में कोई भी गुट सत्ता में आए, वह भारत के हितों का ख्याल रखेगा. दिल्ली के इन कट्टरपंथियों बनाम समझौतावादियों के बीच समानता यही है कि ये दोनों मानते हैं कि अफ़गानिस्तान में प्रतिवादी के तौर पर पाकिस्तान का नज़रिया ही उनकी सोच का आधार है.
भले ही कट्टरपंथी बनाम समझौतावादी भारत की अफ़गानिस्तान के प्रति नीति को प्रभावित करें या नहीं, लेकिन इन तीनों बिंदुओं के मिले-जुले स्वरूप के इर्द-गिर्द ही भारत की नीति घूमती रहती है. इसलिए ये तीनों उपर्युक्त बिंदु ही भारत की अफ़गानिस्तान के प्रति नीति के अनौपचारिक संचालक हैं. नब्बे के दशक के दो विशिष्ट मामले इन गतिशील बिंदुओं की ओर संकेत करते हैं. पहला मामला तब का है जब भारत ने दिल्ली के समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह का तख्ता उलटने के बाद अप्रैल, 1992 में मुजाहिदीन सरकार को मान्यता देने का निर्णय किया था. नीति संबंधी यह परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाकिस्तान पर मुजाहिदीनों की रणनीतिक निर्भरता थी और भारत कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात के संदर्भ में मुजाहिदीनों की जीत को लेकर चिंतित था. परंतु संक्रमण की इस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिलने के कारण और अनेक मुजाहिदीन गुट स्वयं भारत के साथ संबंध बनाने के इच्छुक होने के कारण दिल्ली के समझौतावादी लोगों को अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंधों के बावजूद एक समझौतापरक नीति बनाने में सफलता मिल गई.प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और उनके सक्षम विदेश सचिव के नेतृत्व में यह नीतिगत परिवर्तन लाया जा सका. इसे “राव सिद्धांत” का नाम दिया गया. इसके कारण भारत के लिए मुजाहिदीन गुटों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात के बात करने का रास्ता खुल गया.
दूसरा परिवर्तन सितंबर, 1996 में तब हुआ जब तालिबान काबुल में सत्ता पर काबिज हुए. इस मौके पर समझौते या मिल-जुलकर काम करने की नीति अपनाने के बजाय (मुजाहिदीन की तरह तालिबान ने भी नये चैनल खोलने के लिए दिल्ली से संपर्क करना शुरू कर दिया) भारत ने नई सरकार की आलोचना शुरू कर दी. नीति संबंधी इस परिवर्तन का कारण मात्र यह नहीं था कि तालिबान खूँखार इस्लामी प्रथाएँ अपनाने लगा था या फिर उसकी निर्भरता पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों पर बढ़ने लगी थी, किंतु इन बातों को न केवल मुजाहिदीन के साथ जोड़कर देखा जाने लगा था, बल्कि युद्धरत परस्पर विरोधी विभिन्न गुटों को मनाने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता के कारण नब्बे के दशक के मध्य में अफ़गानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच आम सहमति भी नहीं बन पा रही थी. केवल तीन देशों, पाकिस्तान, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही अफ़गानिस्तान की आधिकारिक सरकार को मान्यता प्रदान की थी. अफ़गानिस्तान की स्थिरता के लिए इसे एक अवसर के रुप में देखने के बजाय रूस और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ इसे एक बढ़ते खतरे के रूप में मान रही थीं और उन्होंने इस पर रोक लगाने का निर्णय किया. क्षेत्रीय भू-राजनैतिक समीकरणों में आए इसी परिवर्तन के कारण दिल्ली के कट्टरपंथी गुट मास्को और तेहरान के साथ मिलकर उनका सहयोग करने लगे और फिर तीनों देशों ने मिलकर तालिबान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का समर्थन शुरू कर दिया. वे अब अमरीका और चीन जैसी उन ताकतों की भी आलोचना करने लगे, जो पर्दे के पीछे रहकर तालिबान को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थीं.
यद्यपि अफ़गानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण भारत के कट्टरपंथियों को एक बार फिर से मौका मिल गया और वे 1996 में आये नीति-संबंधी परिवर्तनों को फिर से लागू करने में जुट गए. मास्को और तेहरान जैसे मित्रदेशों को खोने के डर से समझौतावादी अपने मिशन में कामयाब न हो सके. सन् 1996 में रूस और ईरान दोनों ही संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर भारत के पक्ष का समर्थन करने लगे थे. अगर भारत तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश करता तो भारत इस समर्थन से और अफ़गानिस्तान के अंदर संयुक्त मोर्चे के संबंधों से भी हाथ धो बैठता. इस प्रकार के संवाद को फिर से शुरू करके भारत को “कुछ” तालिबान गुटों का मात्र समर्थन ही पाने की “संभावना” हो सकती थी. सन् 2001 के बाद राष्ट्रपति हमीद कर्ज़ई के शासन-काल में भारत कुछ हद तक नीतिगत दुविधा से बाहर निकल पाया था. कर्ज़ई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से भारत के साथ संबंध बढ़ाये और उन तालिबानी गुटों के साथ भी मेल-मिलाप करने की कोशिश की जिनका पाकिस्तान के साथ मोहभंग होने लगा था.
सन् 2014 में मिली-जुली सेनाओं की वापसी हुई और अशरफ़ घानी ने सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंधों को घटाते हुए पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने पर ज़ोर देना शुरू कर दिया. इसके फलस्वरूप एक बार फिर से हालात बदलने के कारण दिल्ली की नीति में भी परिवर्तन आने लगा. (मास्को सहित) पश्चिमी राजधानियाँ अफ़गानिस्तान में भारत की उपस्थिति के कारण पहले से ही कुछ उलझन महसूस रही थीं. काबुल की वर्तमान सरकार अब चीनी सहयोग से पाकिस्तान की माँगों (इनमें से एक माँग थी, भारत के साथ संबंधों में गिरावट लाने की) का खुशी से समर्थन करने लगी है और भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में भी गिरावट आने लगी है. ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत की रणनीतिक स्थापना में कट्टरपंथियों की धाक बढ़ रही है. जब तक कि आगामी सप्ताहों में कुछ अलग हटकर नहीं होता (जैसे कि घानी पाकिस्तान के साथ शांति-वार्ताएँ बंद कर दें), भारत आधिकारिक तौर पर काबुल के साथ बेरुखी करता रहेगा और साथ ही साथ पर्दे के पीछे उन अफ़गानी गुटों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करता रहेगा जिनके पाकिस्तान के साथ घोषित रूप में शत्रुतापूर्ण संबंध हैं.
अफ़गानिस्तान के प्रति भारत के रुख में पाकिस्तान-विरोधी कट्टरवादिता का पुट अपनाने की रणनीति एक हल्की रणनीति है, जो मतभेदों को कम करने के बजाय पाकिस्तान की असुरक्षा के बिगड़े हुए हालात को और भी बिगाड़ सकती है. समझौतावादी रुख अपनाने से कम से कम क्षेत्रीय संवाद शुरू करने की एक हल्की-सी उम्मीद तो बँधती है. भले ही इस समय उम्मीद की यह किरण कितनी ही धूमिल क्यों न दिखाई पड़ती हो, इससे हिंसा के दुश्चक्र को तोड़ने में मदद ज़रूर मिल सकती है.
पाकिस्तान के साथ शांति-वार्ताओं के काबुल के प्रयोगों को लेकर भारत बस इतना ही कर सकता है कि वह इसके सफल होने की अपनी तमाम आशंकाओं के बावजूद इस पहल का समर्थन तो कर ही सकता है. अल्पकाल में तो इससे अफ़गानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत मिलेगा ही और पाकिस्तान को भी यह संकेत मिलेगा कि अफ़गानिस्तान के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावना हो सकती है और अंततोगत्वा क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए इन देशों के बीच स्थायी संवाद के रास्ते खुलेंगे और इस क्षेत्र में शांति बहाल होगी.
अविनाश पालिवाल लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में रक्षा अकादमी के पोस्ट डॉक्टरल फ़ैलो हैं.
हिंदीअनुवादःविजयकुमारमल्होत्रा, पूर्वनिदेशक(राजभाषा), रेलमंत्रालय, भारतसरकार<malhotravk@gmail.com> / मोबाइल: 91+9910029919.