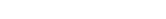सन् 1992 में, जब फ़िल्म इतिहासकार रिचर्ड स्किकेल ने अकादमी पुरस्कार समिति के कहने पर, भारतीय फ़िल्म निर्माता सत्यजीत रे की फ़िल्म क्लिप्स के आधार पर एक मोंताज तैयार किया था, तो उन्हें यू.के. में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और चैनल 4 से फ़ुटेज का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ था.
क्या रे की कृति “relic of a bygone” पहले से ही पुराने ढंग की थी या उसमें सार्वभौमिकता - रे के सिनेमा के एक विशिष्ट मार्कर – के तत्व मौजूद थे, जो उस समय असंभव-से लगते थे?
शायद दूसरी बात ही सही हो. नब्बे के दशक तक रे की फ़िल्में पश्चिम में बहुत कम दिखाई गई थीं. अमेरिकी लेखक और फ़िल्म समीक्षक बर्ट कार्डुलो के अनुसार, रे की कृतियों में निहित मानवतावाद ने उन्हें नुक्सान ही पहुँचाया. "चेखव की तरह रे ने पात्रों या विचारधाराओं के पक्ष में उनका साथ देने से इंकार कर दिया था. क्योंकि उनकी रुचि कुल मिलाकर जटिल मानव में थी. " वह कहा करते थे. "उनकी कृतियों में न तो नायक या खलनायक होता है और न ही कोई साधारण ढंग का विजेता या पराजित होता है. "
रे के नायक केंद्रीय चरित्र होते हैं, जिन्हें अपनी स्थानीय सेटिंग के साथ इस प्रकार के "बुनियादी मानवीय सिद्धांतों" से जुड़ने की स्वतंत्रता होती है, जो "सभी प्रकार की सांस्कृतिक भिन्नताओं को कम करते हुए लगते हैं." दूसरे शब्दों में, रे का सिनेमा मानवीय हालात और "रोज़मर्रे के जीवन की गतिविधियों " - या जीवन के अनाटकीय पहलुओं से उत्पन्न होने वाले भावनात्मक सब्सट्रेट के बारे में होता है.
वैवाहिक
अपूर संसार (1959) में अपू एक आदर्शवादी पात्र है. भाग्य के संयोग से उसकी शादी तय हो जाती है और शादी के दिन ही दूल्हे की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है. वैवाहिक जीवन के लिए तैयार न होने पर भी वह अपने दोस्त की चचेरी बहन अपर्णा से शादी कर लेता है. शुरु-शुरु में अजनबी होने के बावजूद वे जल्द ही प्यार के बंधन में बँध जाते हैं और नवविवाहितों के ठेठ रोमांस से परे वैवाहिक आनंद में डूब जाते हैं.
इस फ़िल्म में रे अपू के जीवन के सवालों के जवाब में प्रेम की अवधारणा का उपयोग पुनर्जीवन के उपकरण के रूप में करते हैं. वह विवाह को कॉमरेडशिप और एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में दिखाते हैं और साथ ही साथ चोरी-छुपी नज़रों की अपनी उदात्त सिनेमाई भाषा के ज़रिये कामुकता की झलक के रूप में शरीर की सूक्ष्म हलचलों को दर्शाते हैं. अपू की यह दुनिया उनकी अगली फ़िल्म देवी में भी जारी रहती है.
देवी (1960) एक ऐसे कट्टर हिंदू ससुर की कहानी है,जो यह मानता है कि उनकी छोटी बहू माँ देवी की अवतार है. यह कहानी बंगाल के उपनिवेशवाद काल के दौरान प्रचलित धार्मिक कट्टरतावाद पर आधारित है. मर्मस्पर्शी छायांकन के माध्यम से युवा दयामयी और उमाप्रसाद की कहानी को दर्शाया जाता है. इसकी शुरुआत कामुकता के पलों से होती है और इसका अंत दुःखद घटनाओं के साथ होता है. आरंभिक दृश्य में दर्शाया जाता है कि 17 वर्षीय दयामयी कामुक भाव से अपने पति के करीब जाने को व्याकुल है, लेकिन उसके पति को अपनी पढ़ाई के लिए कोलकाता लौटना होता है. कैमरे का फ्रेम लकड़ी के बिस्तर पर बनी सेज पर लेटी हुई दयामयी की ओर देखती हुई उमाप्रसाद की नज़रों पर है, लेकिन उनकी नज़रें बिल्कुल नहीं मिलतीं. रे इस ‘नज़र’ तकनीक का उपयोग दर्शकों द्वारा प्रेम की अंतरंगता की कल्पना करने के लिए एक प्रमुख तत्व के रूप में करते हैं.
बाद में, उमाप्रसाद के घर लौटने पर एक ज़रूरी पत्र मिलने के बाद एक दिल दहला देने वाले दृश्य में उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए उसी उपकरण का उलटा उपयोग किया जाता है. जैसे ही वह सजे हुए अपने आँगन में आता है और उसे मानवीय मूर्ति के रूप में कुछ दूरी पर बैठी हुई दयामयी दिखाई देती है और तब वह अपने पति से अपनी नज़रें मिलाती है. वह बेमन से मुस्कुराती है और उसका एक आँसू उसके गाल पर ढुलक आता है. इससे उसकी उलझन, विक्षिप्तता और लाचारी का पता चल जाता है. उमाप्रसाद बहुत कोशिश करता है कि दयामयी देवी के रूप में अपने नए जीवन के पागलपन को समझ जाए, लेकिन वह मना कर देती है. देवी के साथ अपने अनिश्चित वैवाहिक संबंधों और एक बार जुड़े हुए मधुर रिश्ते के टूटने से एक साधारण विवाह के सहज स्वरूप और पितृसत्तात्मक प्रणाली की माँगों के बारे में कुछ खास प्रश्न उठ खड़े होते हैं.
रे की पहली मूल पटकथा, कंचनजंघा (1962) में वर्ग और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से देवी में उठाये गए सवालों को आगे बढ़ाया गया है. कंचनजंघा (1962) में अलग-अलग आयु के तीन विवाहित जोड़ों की कहानी दिखाई गई है, जो दार्जिलिंग में छुट्टियाँ बिताने के दौरान जीवन, शादी, प्यार और बेवफ़ाई के बारे में सोच-विचार करते हैं. आपस में जुड़े इन पात्रों में उनके माता-पिता रायबहादुर इंद्रनाथ राय चौधरी और लाबोन्य, उनकी शर्मीली 19 वर्षीया बेटी मनीषा, उनकी बड़ी बेटी अणिमा और उसके पति शंकर (जिनकी शादी टूटने के कगार पर है), महत्वाकांक्षी इंजीनियर और मनीषा का प्रेमी मुखर्जी और अपने कमजोर मामा के साथ स्वास्थ्य-लाभ के लिए यात्रा पर निकला अशोक नामक एक निम्न मध्यवर्गीय बेरोज़गार आदमी है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मनीषा पहली बार अपने मन की बात बताती है. वह अपने वर्ग की भी परवाह नहीं करती और मुखर्जी के बजाय ज़ाहिर तौर पर अशोक में अधिक दिलचस्पी लेती हुई दिखाई देती है.
मनीषा और अशोक के बीच बढ़ती दिलचस्पी के माध्यम से रे "जैविक" प्रेम की अवधारणा पर लौटते हैं, जैसा कि उन्होंने अपू की दुनिया में किया था. कंचनजंघा में, प्यार सहजता से होता दिखाया गया है और फ़िल्म निर्माता पारंपरिक भागीदारी के आधार पर "परस्पर निर्भरता" का भी परिचय देता है. अणिमा और शंकर के बीच एक तनावपूर्ण दृश्य के दौरान, शंकर अपनी पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ संबंधों को खोल देता है, लेकिन एक-दूसरे पर निर्भर रहने के कारण इसकी परिणति सौहार्द्रपूर्ण सुलह में हो जाती है. वे तलाक का विचार छोड़ देते हैं और इसके बजाय माता-पिता की तरह अपनी छोटी बेटी की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने लगते हैं.
महानगर (1963) में बुनियादी ताने-बाने के रूप में रे की सिनेमाई दृष्टि परस्पर निर्भरता के साथ वैवाहिक संबंधों के शिखर पर पहुँच जाती है. यहाँ एक मध्यमवर्गीय दंपति सुब्रतो और आरती का वैवाहिक जीवन कठोर वास्तविकताओं को न झेल पाने के कारण टूट जाता है. ज़रूरी नहीं कि प्रेम और वैवाहिक संबंध जाहिर तौर पर साथ-साथ चलें, लेकिन फिर भी, रे मर्मस्पर्शी मानवीय संबंधों के टैम्पलेट को अपने सिनेमाई उपकरण के रूप में परस्पर निर्भरता के आधार पर बनाये रखते हैं. इस फ़िल्म में आरती रातों-रात सुब्रतो के बैंक के बंद हो जाने के कारण सेल्सगर्ल की नौकरी करने के लिए विवश हो जाती है.
आरती अपने बड़े परिवार की ज़िम्मेदारी उठाती है और सुब्रतो अपनी पत्नी की नौकरी के लिए आवेदन करने में उसकी मदद करता है. फ़िल्म के अंत में आरती की नौकरी भी छूट जाती है, लेकिन दोनों आशान्वित होकर साथ-साथ रहते हैं. जीवन के प्रति आशावाद के कारण ही रे कहानी में वैवाहिक प्रेम को फिर से लौटा देते हैं. इसके बाद, एक मूल विषय के रूप में "वैवाहिक संबंधों" का फिर से एहसास होता है और राजनीतिक धुरी बन जाती है.
राजनीतिक
रे अपने जीवनी लेखक एंड्र्यू रॉबिन्सन को बताते हैं, "यदि आप एक फ़िल्म निर्माता हैं, तो निश्चित रूप से आपका परिवेश, राजनीति और सभी कुछ सामाजिक परिवेश हो जाता है और यही प्रासंगिक भी हो जाता है. साठ के दशक के बाद से, मैं अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने लगा था.” सामाजिक परिवेश ने बेरोज़गारी और 1970 की राजनीतिक अशांति से संबंधित रे की कृतियों को रे के काम का एक अभिन्न अंग बना दिया था और कोलकोता के लोगों की तकलीफ़ों की परिणति उनकी कोलकोता-त्रयी अर्थात् प्रतिद्वंद्वी (1970), सीमाबद्ध (1971), और जन अरण्य (1975) में हुई थी और यही उनके सबसे निश्चित राजनीतिक सिनेमा बन गए थे.
इन फ़िल्मों के निर्माण के साथ ही रे अब दूर बैठकर पात्रों के जीवन को देखने वाले फ़िल्म निर्माता नहीं रह गए थे, बल्कि अब वह अपने पात्रों के जीवन को नज़दीक से देख रहे थे. उनके शॉट डिविज़न अधिक से अधिक मिड शॉट और क्लोज़-अप के साथ अलग-अलग होने लगे थे, जबकि तंग घर, दफ़्तर और संकरी गलियाँ अब भी उनकी शूटिंग की प्रमुख लोकेशन थीं.
प्रतिद्वंद्वी (1970) में रे ने दृश्यांकन के लिए एक नई सिनेमाई भाषा को अपनाया था. उन्होंने अतीत और चुस्त क्लोज़-अप को फ़िल्म के माध्यम से कलात्मक दिखाने के लिए फ़ोटो निगेटिव का उपयोग किया था. अचानक बोले गए संवाद इस विज़ुअलाइज़ेशन से मेल खाते थे और इस प्रकार एक बेरोज़गार मध्यवर्गीय सिद्धार्थ नामक पात्र को और उसके साथ उसकी दुनिया के डिस्कनेक्ट को कैप्चर कर लिया जाता है. अपनी विधवा माँ के साथ एक तंग किराये के घर में रहते हुए एक क्रांतिकारी भाई-बहन बेहतर जीवन की आकांक्षा रखते हैं और सिद्धार्थ को व्यक्तिगत आकांक्षाओं और बड़े पैमाने पर फैले हुए भ्रष्टाचार के विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
भले ही सिद्धार्थ के जीवन में उदासी के बादल मँडराते रहते हैं, लेकिन रे अपने मुख्य पात्र को मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं. फ़िल्म के मध्य बिंदु पर एक गहन दृश्य में, सिद्धार्थ कोलकाता की भीषण गर्मी में पंखे आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर और इंटरव्यू के लिए घंटों कतार में खड़े बेरोज़गार युवकों की दयनीय स्थिति को लेकर जिस तरह से अपनी भड़ास निकालता है, वह दृश्य बहुत मार्मिक है. कुछ दृश्यों के बाद कीया से अपने प्यार का इज़हार करने के लिए सिद्धार्थ को शब्द नहीं सूझते. वह ज़ाहिर तौर पर कीया को लेकर जिससे वह प्यार करने लगता है, इतना परेशान नहीं है, जितना मताधिकार की धीमी गति का विरोध नहीं कर पाने के कारण परेशान है.
वह शहर,जिसकी स्थापना प्रतिद्वंद्वी (1970) में मनमौजी या बिखरे हुए शहर के रूप में की गई थी, वही जन अरण्य (1975) में कलकत्ता त्रयी के समापन से धूमिल हो जाता है. “मैंने जो एकमात्र धूमिल फ़िल्म बनाई है, वह है, जन अरण्य (1975).“. इस बारे में कोई संदेह ही नहीं है," रे ने 1982 में सिनेस्ट के साथ एक साक्षात्कार में यह कहा था. सोमनाथ मुखर्जी नामक केंद्रीय पात्र, नौकरी तलाशने वाला एक शख्स है. वह फुटबॉल के अपने एक उत्साही साथी बिशु दा से मिलता है. वह उसे एक स्टार्टअप उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है. जल्द ही, सोमनाथ एक महत्वाकांक्षी व्यवसायी के रूप में उभरता हुआ दिखाया गया है. वह अपने खोखले मध्यवर्गीय मूल्यों को छोड़कर व्यापार के खेल के विवादास्पद नियमों को अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है. इस फ़िल्म का अंत प्रतीकात्मक रूप में उसे एक बिचौलिए के रूप में दिखाते हुए होता है, जहाँ वह एक आकर्षक व्यापारिक सौदे के लिए अपने दोस्त की बहन (एक सेक्स वर्कर) के साथ सौदा करते हुए दिखाया जाता है. जन अरण्य (1975) के साथ रे ने "राजनीतिक" के साथ-साथ "वैवाहिक" में निर्देशक के रूप में अपनी यात्रा का समापन किया है, हालाँकि वह बाद की फ़िल्मों में रिश्तों से जुड़े विषयों पर वैसी पोज़ीशनिंग के बिना ही फिर से काम करते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि 1975 तक, हिंदी सिनेमा ने भ्रष्टाचार और विफल होते हुए सिस्टम से निपटना शुरू कर दिया था. उसी साल ‘दीवार’ रिलीज़ हुई थी, जिसे लीक से अलग हटकर एक कल्ट फिल्म माना जाता है. इसी फ़िल्म ने हिंदी सिनेमा के क्रोधित ऐंग्री यंग मैन के किरदार की शुरुआत की थी. प्रतिद्वंद्वी (1970) में सिद्धार्थ क्षणिक रूप में ही अपने मताधिकार से वंचित होने की स्थिति को स्वीकार करता है, और जन अरण्य (1975) में सोमनाथ जीवित रहने के लिए अपनी नैतिकता से समझौता कर लेता है. रे की फ़िल्मों में ये पात्र परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं. इसके विपरीत दीवार और त्रिशूल (1978) में विजय की भूमिकाओं में नायक इनसे बहुत अलग हटकर थे. वे वन-मैन आर्मी की तरह अनिवार्य रूप से न्याय की माँग कर रहे थे. और फिर भी, 48 साल के बाद, रे के "दब्बू" केंद्रीय पात्र, अपू से सोमनाथ तक, अपनी छोटी-बड़ी लड़ाइयों में कहीं अधिक व्यवस्थित और संबद्ध हैं.
नीलोश्री बिस्वास लेखक हैं और साथ ही फ़िल्मनिर्माता भी.
हिंदी अनुवादः डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (हिंदी), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@gmail.com> / Mobile : 91+991002991/WhatsApp:+91 83680 68365