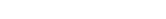भारत में सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच लगभग एक सदी से हिंसक झड़पें होती रही हैं, लेकिन राजनीति-विज्ञानियों, पत्रकारों और भारत के नीति-निर्माताओं का ध्यान इस ओर कम ही गया है. इन लोगों का ध्यान मुख्यतः हिंदू-मुस्लिम दंगों पर ही केंद्रित रहा है. अगर इस तरह की हिंसक झड़पों की उपेक्षा की गई और इनको सुलझाने में देरी की गई तो भारत का सामाजिक ताना-बाना ही बिखर जाएगा. 2020 के दशक तक किसी अन्य देश की तुलना में भारत में मुसलमानों की तादाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए सुन्नी-शिया दंगों को अभी रोकना बेहद ज़रूरी है ताकि भारत का सामाजिक ताना-बाना बिखरने न पाए. इतिहास गवाह है कि सामुदायिक दंगों के कारण भारतीय शहरों का आर्थिक जीवन ठप्प हो जाता है और पहले से ही खस्ता कानून और व्यवस्था की मशीनरी पर उसका बुरा असर पड़ता है.
सामुदायिक हिंसा की समस्या को समझने और उसे सुलझाने का रास्ता लखनऊ से शुरू होता है. लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और भारत के अन्य शहरों के मुकाबले पिछली सदी में हुए अधिकतर सुन्नी-शिया मुसलमानों के दंगों का केंद्रबिंदु भी रहा है. बड़े स्तर पर होने वाले दंगों के कारणों को बदलना तो मुश्किल है, लेकिन मुस्लिम युवाओं के साथ धार्मिक मामलों पर बातचीत करके, उनसे संपर्क बढ़ाकर या उनके विचारों को आमंत्रित करके मुस्लिम मौलवियों से जुड़ी सामुदायिक हिंसा को कम ज़रूर किया जा सकता है.
मामले का चुनाव
सामुदायिक हिंसा के संदर्भ में लखनऊ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो यह उल्लेखनीय है कि सुन्नी और शिया दोनों के लिए ही अन्य भारतीय शहरों की तुलना में मुसलमानों के जीवन की दृष्टि से लखनऊ का ऐतिहासिक,सांस्कृतिक और राजनैतिक कारणों से अधिक महत्व है. शिया लोग लखनऊ पर अपना खास दावा रखते हैं. 1722 से 1856 तक शिया नवाबों ने किस्सों से भरपूर अवध की रियासत पर शासन किया था. कई भारतीय सुन्नी लखनऊ को सम्मान की नज़र से देखते हैं, क्योंकि यह इस्लाम की व्याख्या और अदब का मुख्य स्रोत रहा है और नडवतुल उलेमा जैसे इस्लाम के विश्वविख्यात मदरसे इसकी मिट्टी में ही पनपे हैं और फ़रंगी महल जैसी संस्थाओं की भी यही कार्यस्थली रही है, जिससे निकले अदीबों ने दुनिया-भर में प्रचलित सुन्नी मदरसों की मानक पाठ्यचर्या तैयार की है. लखनऊ के संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ होने वाली सामुदायिक हिंसा पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इसके राजनैतिक मतलब भी हैं. यहाँ लगभग 30 प्रतिशत मतदाता मुसलमान हैं और ध्रुवीकरण की आशंका के कारण उनके वोट का बहुत महत्व है; 60 प्रतिशत लखनवी मुसलमान सुन्नी हैं और 40 प्रतिशत शिया. आखिरकार लखनऊ में होने वाली सामुदायिक हिंसा पर ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लखनऊ में स्थिरता होने पर ही उत्तर प्रदेश में स्थिरता हो पाएगी. इस प्रदेश की आबादी 180 मिलियन है और हिंदू-मुस्लिम दंगों के कारण पहले ही यह प्रदेश काफ़ी पिछड़ चुका है.
हिंसा के कारण
लखनऊ में सुन्नी-शिया दंगों की वारदातें हाल ही में शुरू हुई हैं. पहला दंगा सन् 1905 में हुआ था. आम तौर पर हिंसा का दौर इस्लाम के पवित्र दिनों के दौरान खास तौर पर मुहर्रम के वक्त शुरू होता है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह पहला महीना होता है. इसी दौरान इन समुदायों की अलग-अलग पहचान सामने आती है. मुहर्रम के समय ही मुहम्मद साहब के लाडले पोते हुसैन का सुन्नी खलीफ़ा याज़ीद की फ़ौज ने ईराक़ के कर्बला मैदान में सन् 680 में कत्ल कर दिया था. खास तौर पर शिया समुदाय के लोग हुसैन के कत्ल पर शोक मनाने के लिए एक पवित्र रस्म के तौर पर अपनी छाती पीटते हैं और आत्मबलिदान की कोशिश करते हैं. शिया लोग मुहर्रम की रस्म के तौर पर चौथे खलीफ़ा और हुसैन के अब्बा हुज़ूर अली की मौत का भी शोक मनाते हैं. शिया लोग पहले तीन खलीफ़ाओं को वैधता को स्वीकार नहीं करते. उनके अनुसार अली ही असली उत्तराधिकारी है, क्योंकि स्वयं मुहम्मद ने उसका चुनाव किया था. इससे दोनों समुदायों के बीच मतभेद बढ़ने की पूरी गुंजाइश है.
सन् 1905 में हिंसा तब भड़की थी, जब एक सुन्नी मौलवी ने एक युवक को शियाओं के एक जुलूस के पास पहले तीन खलीफ़ाओं (मध-ए-सहाबा) की तारीफ़ में भड़काऊ गीत गाने को कहा. इसके उत्तर में शियाओं ने पहले तीन खलीफ़ाओं (तबर्रा) को कोसते हुए गीत गाए. लखनऊ में मध-ए-सहाबा और तबर्रा गाते हुए ही हिंसा भड़कने लगती है.
समाज विज्ञान के नज़रिये से लखनऊ की सामुदायिक हिंसा की शुरुआत होने और आज भी उसके जारी रहने के कुछ अंदरूनी कारण हैं. कुछ समाज विज्ञानियों के अनुसार पहला कारण तो यह है कि एक जातीय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की जाने वाली राजनीति में अंतर्जातीय हिंसा का जोखिम बना रहता है, क्योंकि जातीय बहुसंख्यक समुदाय की धारणा बनी रहती है कि मात्र संख्या बल अधिक होने के कारण उन्हें बहिष्कृत करना जायज़ नहीं है. जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के नियमों को कुछ हद तक तो गृह युद्ध से जोड़कर देखा ही जा सकता है. इस तर्क के मद्देनज़र लखनऊ में सामुदायिक हिंसा का जोखिम हमेशा ही बना रहा है, क्योंकि सुन्नी बहुसंख्यक समुदाय को दो सदियों तक चलने वाले अल्पसंख्यक शिया शासन के दौरान अधिकतर राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के दायरे से बाहर रखा जाता रहा है. अब तक हाशिये पर रहने के कारण उनकी आमदनी भी एक वजह है, जिसके कारण दंगे भड़कते रहे हैं. इतिहासकारों ने लिखा है कि ब्रिटिश द्वारा सन् 1856 में लखनऊ के अंतिम बादशाह को सत्ता से बेदखल करने के बाद से ही औसत सुन्नियों की आमदनी बढ़ती रही है और औसत शियाओं की आमदनी घटती रही है या फिर स्थिर रही है.
समाज विज्ञानियों के अनुसार दूसरा कारण यह है कि तथाकथित “जातीय उद्यमकर्ताओं” द्वारा भी जातीय हिंसा भड़काने की संभावना हो सकती है. इनका प्रयास यही रहता है कि सह-जातीय समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक पूरी रणनीति के तहत दोनों समुदायों के मदभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाए और दूसरे समुदाय को एक खतरे के रूप में दिखाया जाए. ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है कि धार्मिक उद्यमकर्ता ही लखनऊ और उसके आस-पास के इलाकों में हिंसा भड़काने के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सुन्नी देवबंदी और बरेलवी जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलनों की पैदाइश के बाद कई सुन्नी मौलवियों ने कट्टर इस्लामी सिद्धांतों को प्रचारित करना शुरू कर दिया था और शिया समुदाय के मत का और मुहर्रम के समय शोक मनाने की उनकी रस्म का भी वे धर्मशास्त्र की दृष्टि से खंडन करने लगे थे. कुछ शिया मौलवी भी अपने अनुयायियों को भड़काने लगे थे कि सुन्नियों के कारण भारत और विदेशों में शिया मत पर खतरा मंडरा रहा है. धार्मिक उद्यमकर्ताओं की ये कोशिशें आज भी जारी हैं, जिसके कारण लखनवी मौलाना और राजनीतिज्ञ शिया और सुन्नी मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके ध्रुवीकरण के मकसद से उनमें भय का उन्माद पैदा कर रहे हैं.
हस्तक्षेप
लखनऊ के मुस्लिम समुदायों में अधिकाधिक सार्वजनिक निवेश जैसे बड़े नीतिगत सुधारों से सामुदायिक संघर्ष को हवा देने वाली आर्थिक दिक्कतों को कम किया जा सकता है, लेकिन निकट भविष्य में तो ऐसे सुधारों की उम्मीद नहीं है और इनसे पूर्वाग्रहों और हिंसा भड़काने वाले कारणों को भी दूर नहीं किया जा सकेगा. यह तभी संभव है जब स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और लखनऊ के कुछ सहिष्णु सुन्नी और शिया मौलवी अपने युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम शुरू करें जिनकी मदद से पूर्वाग्रहों और हिंसा का समर्थन करने वाले तत्वों को दूर किया जा सके. इन कार्यक्रमों का मकसद होगा, जातीय उद्यमकर्ताओँ द्वारा की जाने वाली सामुदायिक अपील के प्रभाव को कम करना.
मनोवैज्ञानिक शोध के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने चाहिए. यद्यपि हिसा के वातावरण में पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए प्रायोगिक साक्ष्यों की कमी है, फिर भी सामाजिक मनोविज्ञान के तीन उपायों को अपनाने से आशा की किरण फूटने की उम्मीद की जा सकती है.
एक उपाय तो यही है कि व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें समझाया जाए कि ये पूर्वाग्रह उनके धार्मिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं. संज्ञानपरक असंगति सिद्धांत और मूल्य आधारित आत्मविरोधी रवैये के आधार पर ऐसे हस्तक्षेपों में इमामों को भी शामिल किया जाए ताकि वे अपने समुदाय के युवाओं को समझाएँ कि ऐसे पूर्वाग्रह उनके अपने धार्मिक मूल्यों के खिलाफ़ हैं. अमरीका में किये गये प्रायोगिक साक्ष्य से पता चलता है कि मूल्य आधारित आत्मविरोधी रवैये से कुछ अधिक समय में रंगभेद, लैंगिक और परिवेशगत पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये को बदला जा सकता है.
दूसरे उपाय में विस्तारित संपर्क अनुमान शामिल है, जिसे अमरीका में लैब और फ़ील्ड में किये जा रहे प्रयोगों से मदद मिलती है. सुन्नी और शिया युवाओं को सीधे एक-दूसरे से मिलाने के बजाय इस उपाय के अंतर्गत प्रत्येक समुदाय का अलग समूह बनाया जाता है. व्यक्तिगत स्तर पर लोग अंतःसमूह के उन सदस्यों के माध्यम से बाह्यसमूह के बारे में सकारात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं जिनके बाह्यसमूह के सदस्यों के साथ उनके अच्छे दोस्ताना संबंध होते हैं. बाह्यसमूह के सदस्यों के सकारात्मक असर के कारण सारे ही बाह्यसमूह के पूर्वाग्रह कुछ कम हो सकते हैं. यहाँ बर्ताव में तबदीली दो कारणों से हो सकती है. बाह्यसमूह की विशेषताओं के मूल्यांकन में बदलाव आने के कारण या उस धारणा में बदलाव आने के कारण कि बाह्यसमूह के प्रति पूर्वाग्रह सामाजिक दृष्टि से अपेक्षित है.
अंतिम हस्तक्षेप तभी कारगर होता है जब बाह्यसमूह के लिए समझ-बूझ को प्रोत्साहन दिया जाता है. इस प्रक्रिया का समर्थन अमरीका की प्रयोगशालाओं में किये गये परीक्षणों से भी होता है. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ऐसा हस्तक्षेप तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक समुदाय के प्रतिभागियों को धारणा बनने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए. यह एक ऐसी मानक गतिविधि है, जिससे पूर्वाग्रह कम करने में और बर्ताव को सुधारने में मदद मिलती है. प्रत्येक प्रतिभागी निजी तौर पर बाह्यसमूह के सदस्य के नज़रिये से एक पृष्ठ में लिखेगा कि वह प्रतिभागी के धार्मिक समूह के सदस्य से भेदभाव किये जाने पर कैसा महसूस करेगा.
मुख्य मार्ग पर चलना
इन उपायों में से समझाने-बुझाने का काम सहिष्णु मौलवियों के द्वारा सहभागिता की माँग करते समय कितना भी निराशाजनक क्यों न लगे, लेकिन यही एक उपाय है जो हिंसा के धार्मिक उन्माद को कम करने में सीधे ही कारगर हो सकता है. संपर्क बढ़ाने का उपाय भी तार्किक दृष्टि से संभव लगता है, क्योंकि उसमें धार्मिक संस्थाओं की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके लिए ऐसे सहिष्णु युवाओं की आवश्यकता होती है, जो अंतःसमूह के सदस्यों को अपना दृष्टिकोण समझाने को इच्छुक हों. धारणा स्वीकार करने का विकल्प भी तार्किक दृष्टि से सबसे अधिक संभव लगता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रतिभागी इस प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें, लेकिन इस प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को समर्थन देने वाले सामाजिक दबाव को कम करने में प्रतिभागी की कोई खास मदद नहीं मिलती.
लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के नेताओं को ऐसे कम खर्चीले हस्तक्षेपों की व्यवस्था करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन मिल सकते हैं. यदि कुछ सुन्नी और शिया इमाम दोनों समुदायों के बीच की दरार को कम करने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं तो शहर के उन मुसलमानों का उन्हें व्यापक समर्थन मिल सकता है जो राजनैतिक और वित्तीय लाभ पाने के इच्छुक मौलवियों से बहुत प्रभावित नहीं होते. लखनऊ का अनौपचारिक कारोबार और नागरिक संगठन खुले तौर पर उनका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि निचले स्तर पर होने वाले सामुदायिक संघर्ष से सरकारी और निजी निवेश मिलने के कारण शहर के मुसलमानों को आर्थिक तौर पर लाभ मिल सकता है. लगातार सही नेतृत्व मिलने पर शांति सभी के लिए लाभदायक हो सकती है.
कुनाल शर्मा कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में डॉक्टरेट के प्रत्याशी हैं.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@gmail.com> / मोबाइल : 91+9910029919